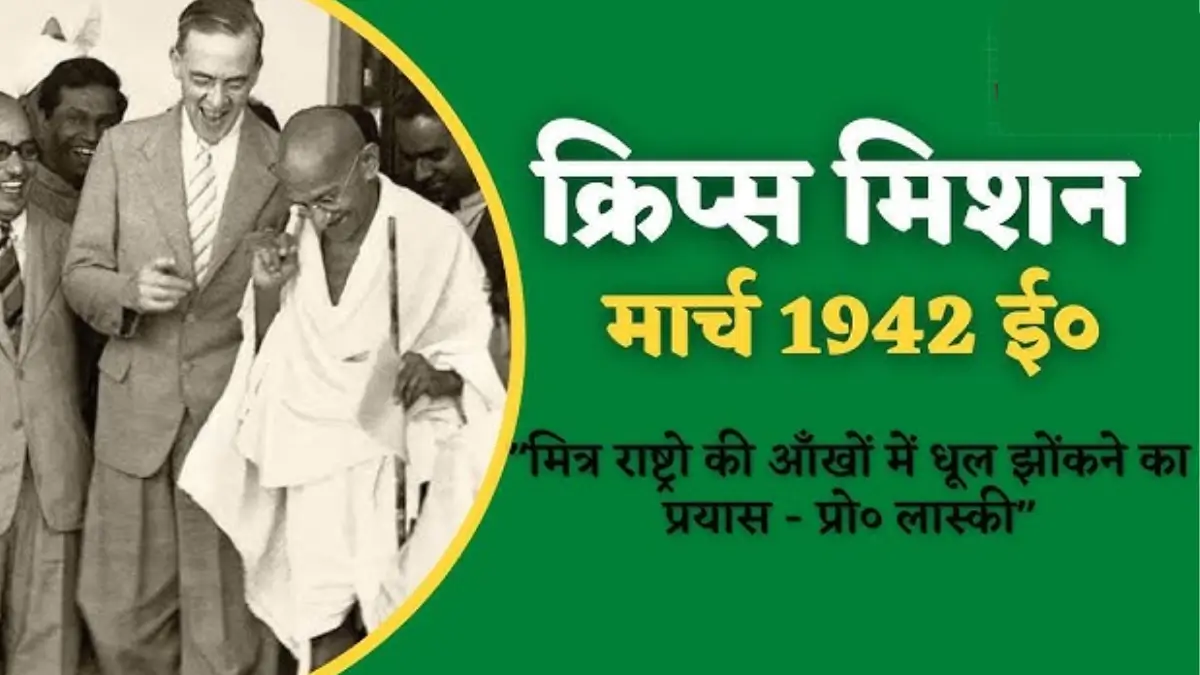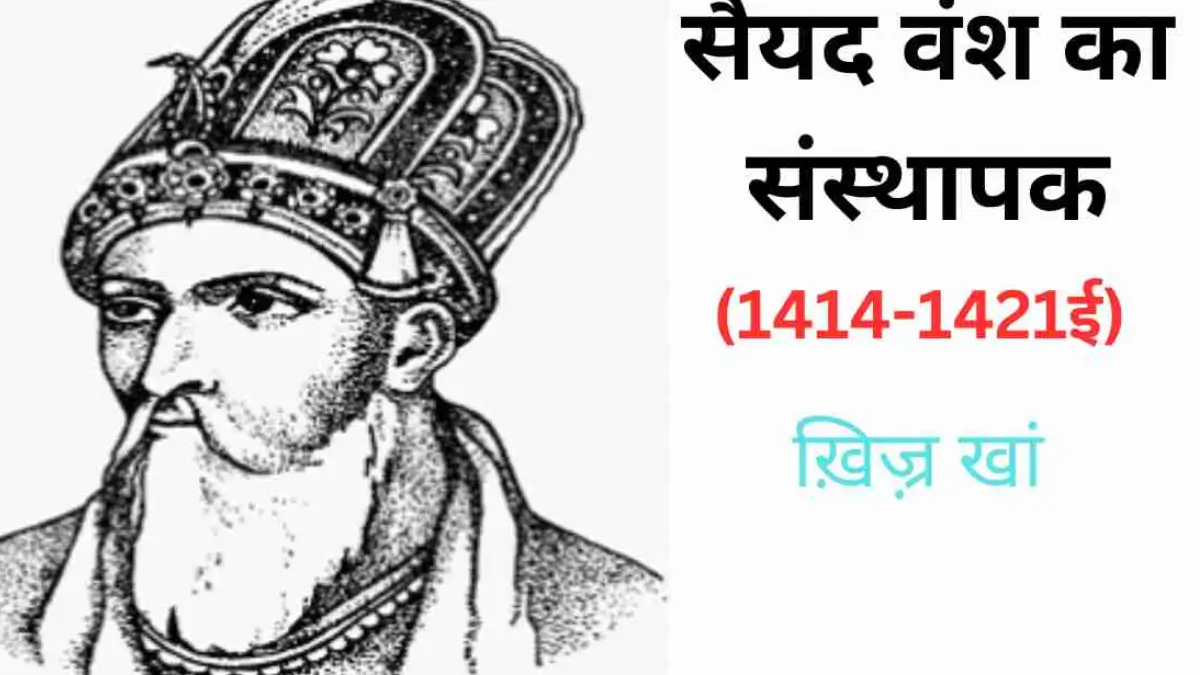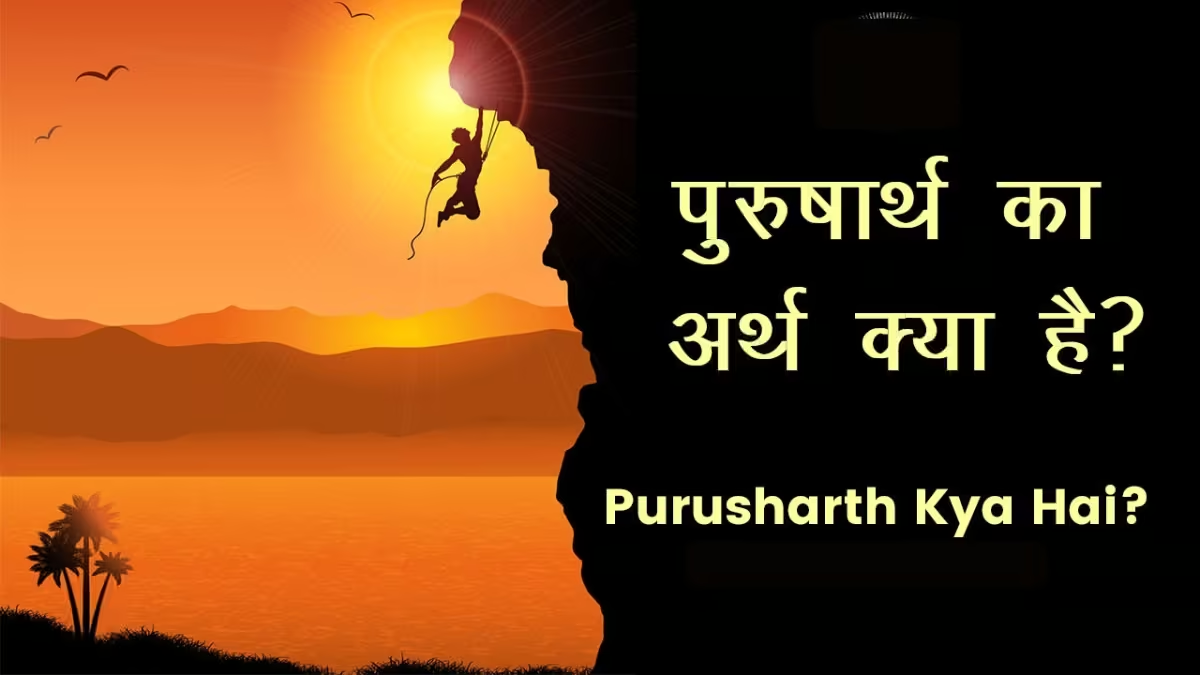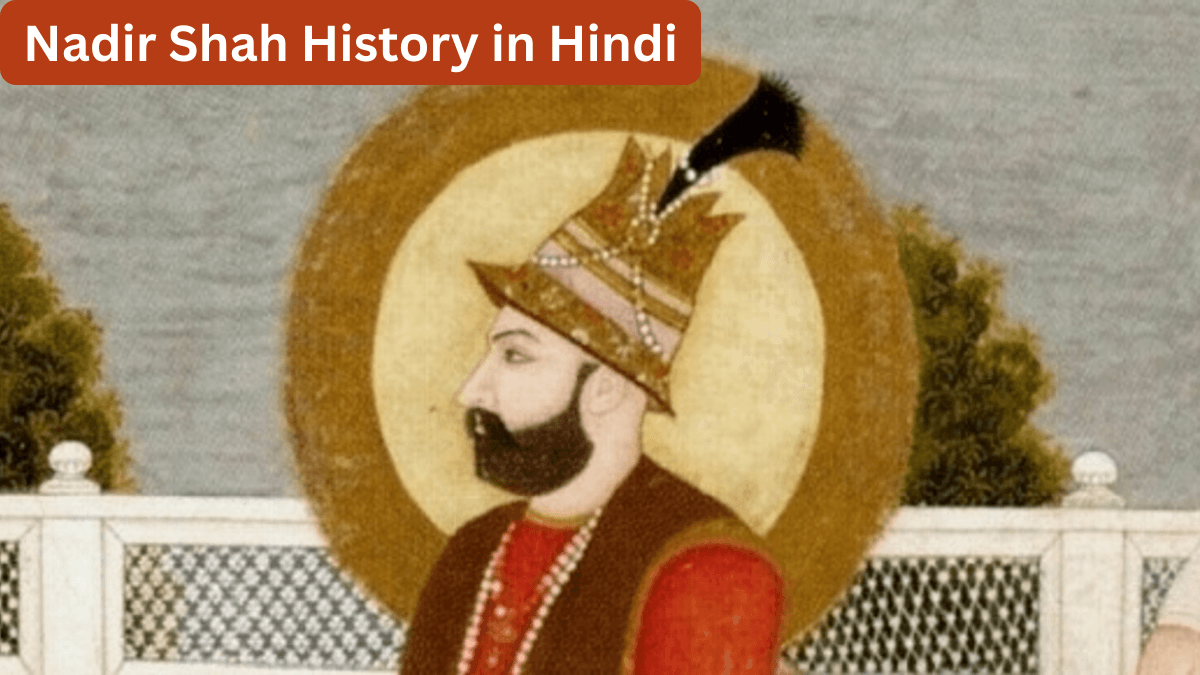Non-Cooperation Movement: असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध को जन-आंदोलन का रूप दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1922 तक चला यह आंदोलन भारतीयों में स्वराज्य और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में सफल रहा। यह लेख असहयोग आंदोलन के विभिन्न पहलुओं जैसे इसके कारण, शुरुआत, विस्तार, नेतृत्व, प्रभाव, समाप्ति और असफलता के कारणों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
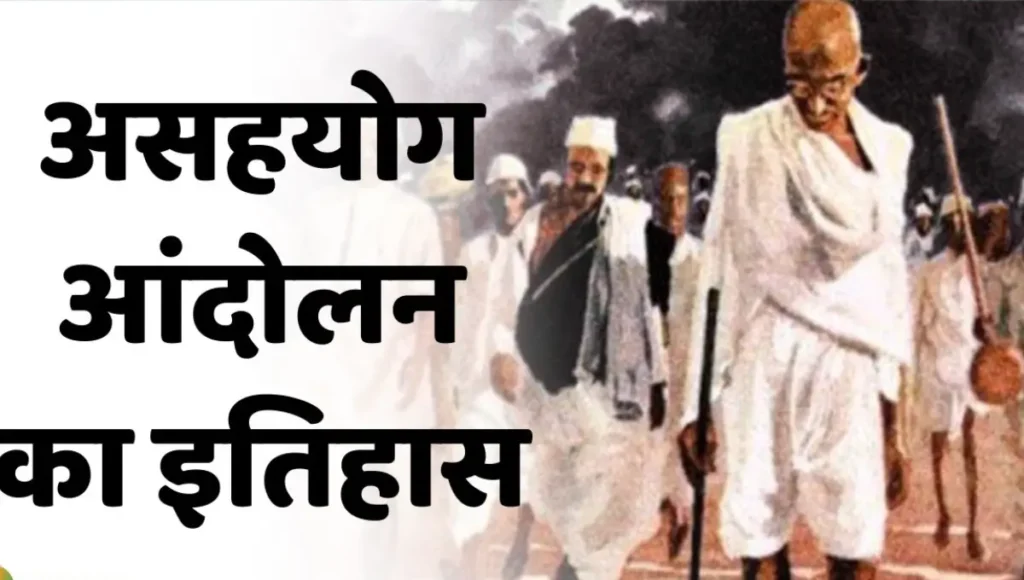
Non-Cooperation Movement: असहयोग आंदोलन की टाइमलाइन
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| समयावधि | 1 अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक। औपचारिक शुरुआत: सितंबर 1920 (कलकत्ता अधिवेशन), समाप्ति: 12 फरवरी 1922 (चौरा चौरा घटना के बाद)। |
| प्रमुख कारण | 1. रॉलेट एक्ट (1919): बिना मुकदमे गिरफ्तारी की अनुमति। 2. जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919): निहत्थों पर गोलीबारी। 3. हंटर कमीशन की विफलता: हल्की सजा। 4. खिलाफत आंदोलन: खलीफा के मुद्दे पर मुस्लिम असंतोष। 5. मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919): अपर्याप्त स्वशासन। 6. आर्थिक संकट: महंगाई, भारी कर, कृषि-उद्योग में गिरावट। |
| शुरुआत का स्थान | कलकत्ता (कोलकाता), सितंबर 1920 (कांग्रेस अधिवेशन); नागपुर, दिसंबर 1920 में औपचारिक स्वीकृति। |
| प्रमुख कार्यकर्म | 1. ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और नौकरियों का बहिष्कार। 2. विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, खादी और स्वदेशी का प्रचार। 3. करों का भुगतान न करना। 4. हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन। 5. शांतिपूर्ण हड़तालें और प्रदर्शन। 6. सविनय अवज्ञा की योजना (1921, अहमदाबाद अधिवेशन)। |
| प्रमुख नेता | – महात्मा गांधी: अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर नेतृत्व। – अली बंधु (मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली): खिलाफत आंदोलन के नेता। – मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू: कांग्रेस के प्रमुख समर्थक। |
| विस्तार | – शहरी क्षेत्र: मध्यम वर्ग, छात्रों और वकीलों की भागीदारी; विदेशी सामान की होली। – ग्रामीण क्षेत्र: अवध (किसान विद्रोह), मालाबार (मोपला विद्रोह), असम (चाय बागान हड़ताल), आंध्र (वन कानून उल्लंघन), पंजाब (अकाली आंदोलन)। – 1921 में 396 हड़तालें, 6 लाख श्रमिक, 70 लाख का नुकसान। |
| प्रभाव | – राष्ट्रीय जागरण: लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। – आर्थिक प्रभाव: विदेशी कपड़ों का आयात 50% कम। – सामाजिक एकता: हिंदू-मुस्लिम एकता (मोपला विद्रोह अपवाद)। – महिलाओं की भागीदारी: प्रदर्शन और पिकेटिंग में सक्रियता। – राजनीतिक प्रभाव: कांग्रेस मजबूत, ब्रिटिश शासन हिला। – नकारात्मक प्रभाव: हिंसक घटनाएं (मोपला, चौरा चौरा)। |
| समाप्ति | – तिथि: 12 फरवरी 1922 (बारडोली बैठक)। – कारण: चौरा चौरा घटना (4 फरवरी 1922, 22 पुलिसकर्मियों की हत्या)। – गांधीजी की गिरफ्तारी: 10 मार्च 1922, 6 साल की सजा (1924 में रिहा)। |
| असफलता के कारण | 1. स्वराज का लक्ष्य अधूरा। 2. मध्यम वर्ग की सीमित भागीदारी (खादी महंगी)। 3. क्षेत्रीय भिन्नताएं। 4. ब्रिटिश दमन। 5. हिंसक घटनाएं (मोपला, चौरा चौरा)। 6. नेताओं में मतभेद (मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की आलोचना)। |
| गांधीजी का लंगोटी धारण | – कब: 22 सितंबर 1921, मदुरै (मद्रास)। – कारण: गरीब जनता के साथ एकरूपता, स्वदेशी का प्रचार, सादगी और अहिंसा का संदेश। – प्रभाव: गांधीजी को “आम आदमी का नेता” बनाया, स्वदेशी को बढ़ावा। |
| प्रमुख घटनाएं | – जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919) के विरोध में शुरू। – प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार (17 नवंबर 1921, काले झंडे, हड़ताल)। – चौरा चौरा हिंसा (4 फरवरी 1922)। |
| नेताओं की प्रतिक्रियाएं | – मोतीलाल नेहरू: “एक गाँव की हिंसा के लिए पूरे देश को सजा क्यों?” – सुभाष चंद्र बोस: “वापसी राष्ट्रीय दुर्भाग्य।” |
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ?
असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता (कोलकाता) अधिवेशन में इसे स्वीकृति मिली, और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसे और मजबूती प्रदान की गई। यह आंदोलन जनवरी 1921 से पूरे देश में जोर पकड़ने लगा और फरवरी 1922 तक चला, जब चौरा चौरा की हिंसक घटना के बाद इसे स्थगित कर दिया गया।

असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण
असहयोग आंदोलन की शुरुआत के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे।यहाँ हम निम्नलिखित छह प्रमुख कारण प्रस्तुत कर रहे हैं:
- रॉलेट एक्ट (1919): ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके तहत बिना पूर्व सूचना के और बिना दलील तथा मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने की अनुमति थी। इस दमनकारी कानून ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ाया।
- जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919): 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया।
- हंटर कमीशन की विफलता: जलियांवाला बाग की जांच के लिए गठित हंटर कमीशन ने जनरल डायर को मामूली सजा दी, जिससे भारतीयों का ब्रिटिश न्याय पर भरोसा टूटा।
- खिलाफत आंदोलन: प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन और खलीफा के मुद्दे पर ब्रिटिश नीतियों से मुसलमानों में नाराजगी थी। गांधी ने इसे समर्थन देकर हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया।
- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की नाराजगी: 1919 के सुधार भारतीयों की स्वराज की मांग को पूरा नहीं कर सके, जिससे राजनीतिक निराशा बढ़ी।
- आर्थिक संकट: प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई, भारी कर और कृषि-उद्योगों में गिरावट ने जनता को आर्थिक रूप से परेशान किया, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह बढ़ा।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई?
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कोलकाता में सितंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन से हुई। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी ने इसे औपचारिक रूप दिया। जनवरी 1921 से यह आंदोलन देशभर में फैल गया। शुरू में यह शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित था, लेकिन जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और आदिवासियों तक इसका प्रभाव पहुंचा।
यह भी भी पढ़िए
| 1857 की क्रांति के कारण, घटनाएं, परिणाम, नायक | भगत सिंह का जीवन परिचय: जन्मदिन, स्वतंत्रता संग्राम, |
| क्रिप्स मिशन इन हिंदी, उद्देश्य, प्रस्ताव | लाल बहादुर शास्त्री जीवनी: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री |
असहयोग आंदोलन में गांधीजी के कर्यक्रम
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक और रचनात्मक प्रतिरोध के रूप में संगठित किया। उनके कार्यकर्म निम्नलिखित थे:
- ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार:
- शैक्षिक संस्थाएं: गांधीजी ने भारतीयों से ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को बढ़ावा दिया, जैसे काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ।
- न्यायालय: वकीलों से ब्रिटिश अदालतों में काम बंद करने को कहा गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी।
- सरकारी नौकरियां और सम्मान: सरकारी नौकरियों और ब्रिटिश उपाधियों (जैसे राय बहादुर, नाइटहुड) को त्यागने का आग्रह किया गया। रवींद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी।
- करों का बहिष्कार: गांधीजी ने लोगों से ब्रिटिश करों का भुगतान न करने का आह्वान किया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- स्वदेशी और खादी का प्रचार:
- गांधीजी ने विदेशी सामान, विशेष रूप से ब्रिटिश कपड़ों, का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से खादी पहनने और चरखा चलाने का आग्रह किया, जिससे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया। 1921-1922 में विदेशी कपड़ों का आयात 50% कम हुआ।
- यह कार्यकर्म आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वराज की नींव रखने के लिए था। गांधीजी ने स्वयं खादी पहनना शुरू किया और इसे भारतीय पहचान का प्रतीक बनाया।
- हिंदू-मुस्लिम एकता और खिलाफत आंदोलन का समर्थन:
- गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा की स्थिति को पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहा था। अली बंधु (मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली) के साथ मिलकर गांधीजी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।
- इस गठजोड़ ने असहयोग आंदोलन को व्यापक जन-आधार दिया, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त हुआ।
- हड़तालें और प्रदर्शन:
- गांधीजी ने शांतिपूर्ण हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका काले झंडों से विरोध और हड़ताल के साथ स्वागत किया गया।
- शहरों में दुकानें बंद रहीं, और मजदूरों ने हड़तालें कीं। 1921 में 396 हड़तालों में 6 लाख से अधिक श्रमिक शामिल हुए, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को 70 लाख का नुकसान हुआ।
- रचनात्मक कार्यकर्म:
- गांधीजी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया, जैसे हरिजन उद्धार, शिक्षा का प्रसार, और ग्रामीण स्वच्छता। ये कार्यकर्म स्वराज के लिए जनता को तैयार करने के लिए थे।
- उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के प्रशिक्षण पर बल दिया ताकि आंदोलन हिंसक न हो।
- सविनय अवज्ञा की योजना:
- दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गांधीजी ने असहयोग को और तेज करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि, यह चौरा चौरा घटना के कारण लागू नहीं हो सका।
गांधीजी ने पहली बार लंगोटी कब धारण की?
महात्मा गांधी ने पहली बार लंगोटी (धोती या न्यूनतम खादी वस्त्र) को अपनी पहचान के रूप में 22 सितंबर 1921 को मदुरै (मद्रास, अब तमिलनाडु) में धारण किया। यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, जब वे स्वदेशी और सादगी को बढ़ावा दे रहे थे। इस घटना का ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व था।
लंगोटी धारण करने के कारण:
- भारतीय जनता के साथ एकरूपता: गांधीजी ने देखा कि भारत के गरीब किसान और मजदूर न्यूनतम कपड़े पहनते हैं। लंगोटी धारण करके वे भारत की गरीब जनता के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा, “मैं उस भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ जो गरीब और वंचित है।”
- स्वदेशी का प्रतीक: लंगोटी खादी से बनी थी, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक थी। यह विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और भारतीय हस्तनिर्मित कपड़ों को अपनाने का संदेश देता था।
- सादगी और अहिंसा का संदेश: गांधीजी का मानना था कि सादगी और आत्म-अनुशासन स्वराज की नींव हैं। लंगोटी उनकी अहिंसक और न्यूनतम जीवनशैली का प्रतीक बन गई।
- ब्रिटिश शासन को चुनौती: लंगोटी धारण करके गांधीजी ने ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक संस्कृति और भौतिकता को चुनौती दी। यह एक तरह का सांस्कृतिक और वैचारिक विरोध था।
लंगोटी धारण की घटना:
- स्थान और समय: मदुरै में 22 सितंबर 1921 को एक सभा के दौरान गांधीजी ने केवल एक छोटी धोती (लंगोटी) और चादर पहनने का फैसला किया। इससे पहले वे पूर्ण धोती और कुर्ता पहनते थे।
- प्रभाव: इस निर्णय ने जनता में गहरा प्रभाव डाला। लोगों ने इसे उनकी सादगी और भारतीयता का प्रतीक माना। यह स्वदेशी आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने वाला कदम था।
- विवाद: कुछ समकालीन नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसे अतिशयोक्ति माना, लेकिन गांधीजी ने इसे अपनी विचारधारा का हिस्सा बनाया।
असहयोग आंदोलन का विस्तार
असहयोग आंदोलन ने भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को एकजुट किया। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित थे:
- शहरी क्षेत्र:
- छात्रों ने ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया।
- वकीलों ने अदालतों में काम करना बंद कर दिया।
- विदेशी कपड़ों को जलाकर खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया।
- कई शहरों में हड़तालें और प्रदर्शन हुए।
- ग्रामीण क्षेत्र:
- अवध (उत्तर प्रदेश): किसानों ने जमींदारों और ब्रिटिश करों के खिलाफ विद्रोह किया।
- मालाबार (केरल): मोपला मुस्लिम किराएदारों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया, जो बाद में सांप्रदायिक रूप ले लिया।
- असम: चाय बागान मजदूरों ने हड़तालें कीं।
- आंध्र प्रदेश: वन कानूनों का उल्लंघन हुआ।
- पंजाब: अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों को मुक्त करने का प्रयास किया।
1921 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 396 हड़तालों में 6 लाख से अधिक श्रमिक शामिल हुए, जिससे 70 लाख का आर्थिक नुकसान हुआ। यह आंदोलन पहली बार शहरी और ग्रामीण भारत को स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट करने में सफल रहा।
असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता
असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर इसे संचालित किया। अन्य प्रमुख नेता शामिल थे:
- अली बंधु (मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली): खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, जिन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ाया।
- मोतीलाल नेहरू: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने आंदोलन को संगठित किया।
- चित्तरंजन दास: बंगाल में आंदोलन को गति दी।
- लाला लाजपत राय: पंजाब में आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया।
- जवाहरलाल नेहरू: युवा नेतृत्व के रूप में उभरे।
असहयोग आंदोलन का प्रभाव
असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डाला। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे:
- राष्ट्रीय चेतना का प्रसार: यह पहला जन-आधारित आंदोलन था, जिसने मध्यम वर्ग, किसानों, मजदूरों और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा।
- आर्थिक प्रभाव: विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से आयात में 50% की कमी आई। खादी और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला।
- सामाजिक एकता: हिंदू-मुस्लिम एकता मजबूत हुई, हालांकि मोपला विद्रोह जैसे कुछ अपवाद रहे।
- महिलाओं की भागीदारी: महिलाओं ने प्रदर्शन, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई।
- राजनीतिक प्रभाव: ब्रिटिश शासन की नींव हिली, और कांग्रेस एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरी। यह भविष्य के आंदोलनों की नींव बना।
- नकारात्मक प्रभाव: मोपला विद्रोह और चौरा चौरा जैसी हिंसक घटनाओं ने मध्यम वर्ग को चिंतित किया और आंदोलन को कमजोर किया।
असहयोग आंदोलन की समाप्ति
असहयोग आंदोलन की समाप्ति फरवरी 1922 में हुई, जब महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया। इसका मुख्य कारण 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरा की हिंसक घटना थी, जिसमें गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यह घटना गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध थी। गांधी ने कहा कि सत्याग्रहियों को और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मार्च 1922 में गांधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर छह साल की सजा दी गई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया।
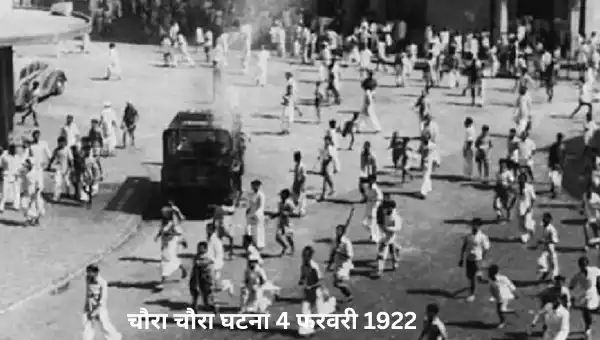
असहयोग आंदोलन क्यों असफल रहा और क्यों स्थगित किया गया?
स्थगन के कारण:
- चौरा चौरा घटना: 4 फरवरी 1922 को हुई हिंसा ने गांधी को आंदोलन स्थगित करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे हिंसक आंदोलन नहीं चाहते थे।
- अहिंसा का सिद्धांत: गांधी का मानना था कि हिंसा से आंदोलन का उद्देश्य भटक जाएगा।
असफलता के कारण:
- स्वराज का लक्ष्य अधूरा: एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।
- मध्यम वर्ग की सीमित भागीदारी: खादी महंगी थी, और स्वदेशी विकल्प अपर्याप्त थे।
- क्षेत्रीय भिन्नताएं: कई क्षेत्रों में आंदोलन स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहा।
- ब्रिटिश दमन: नेताओं की गिरफ्तारी और सरकारी दमन ने आंदोलन को कमजोर किया।
- हिंसक घटनाएं: मोपला विद्रोह और चौरा चौरा ने आंदोलन की विश्वसनीयता को प्रभावित किया।
- आंतरिक मतभेद: कुछ नेताओं, जैसे सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, ने स्थगन के निर्णय की आलोचना की।
नेताओं की प्रतिक्रियाएँ
आंदोलन के स्थगन पर कई नेताओं ने असहमति जताई। मोतीलाल नेहरू ने कहा, “यदि एक गाँव अहिंसा का पालन नहीं करता, तो पूरे देश को सजा क्यों?” सुभाष चंद्र बोस ने इसे “राष्ट्रीय दुर्भाग्य” बताया, क्योंकि जनता का उत्साह चरम पर था। इन मतभेदों ने गांधी की लोकप्रियता पर असर डाला, लेकिन उनकी अहिंसा की प्रतिबद्धता अटल रही।
असहयोग आंदोलन में गांधीजी की भूमिका
चौरा चौरा और स्थगन: 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरा में हिंसक घटना (22 पुलिसकर्मियों की हत्या) के बाद गांधीजी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा, “सत्याग्रहियों को और प्रशिक्षण की जरूरत है।” यह निर्णय विवादास्पद रहा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसे जल्दबाजी माना।
नेतृत्व और संगठन: गांधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्गठित किया और इसे जन-आधारित संगठन बनाया। उन्होंने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को संगठित किया।
अहिंसा और सत्याग्रह: गांधीजी ने अहिंसा को आंदोलन का मूल सिद्धांत बनाया। उन्होंने लोगों को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित किया, ताकि वे शांतिपूर्ण प्रतिरोध कर सकें।
जन-जागरण: गांधीजी ने देशभर में यात्राएं कीं, सभाएं कीं और स्वदेशी, स्वराज और एकता का संदेश दिया। उनकी सादगी और नैतिक बल ने लाखों लोगों को प्रेरित किया।
निष्कर्ष
असहयोग आंदोलन भले ही स्वराज प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ाया, स्वदेशी और खादी को प्रोत्साहन दिया, और लाखों भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। चौरा चौरा जैसी घटनाओं ने इसे स्थगित कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव भविष्य के आंदोलनों, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, में स्पष्ट दिखाई दिया। यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।