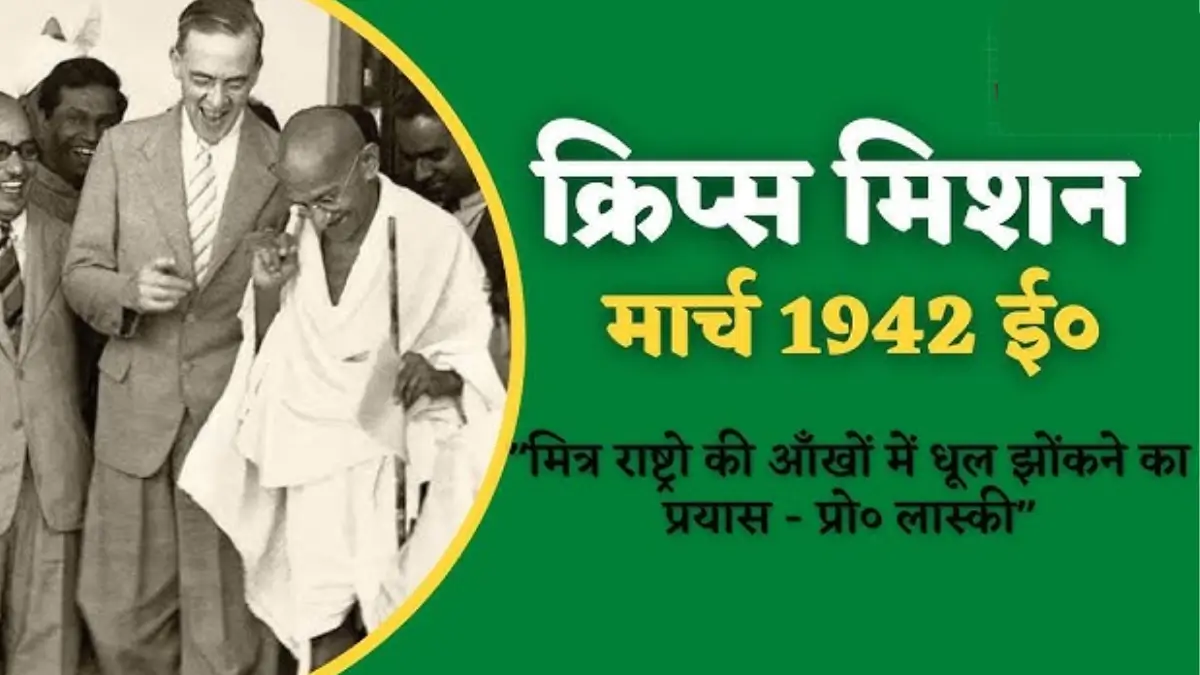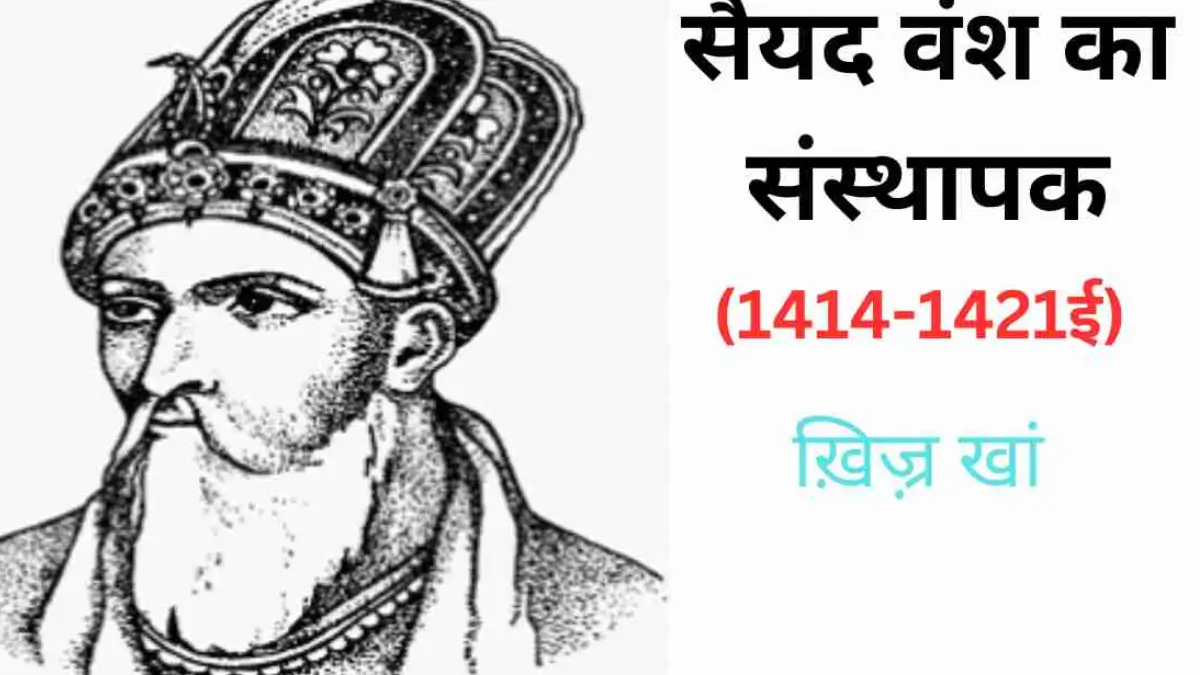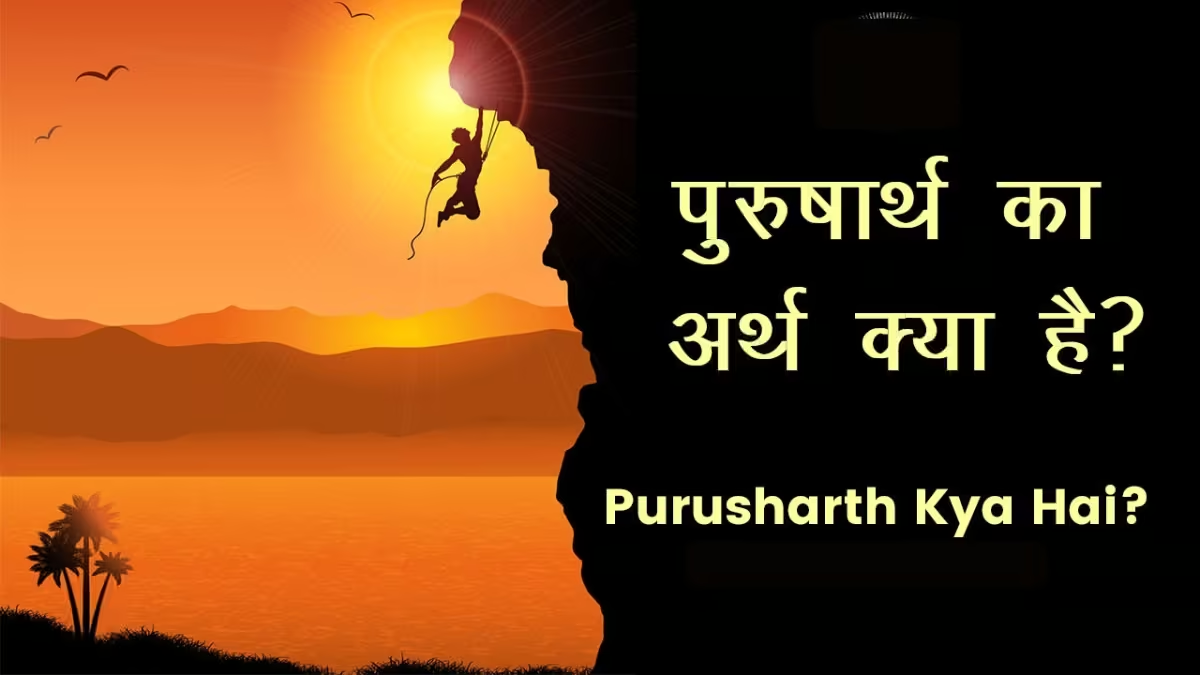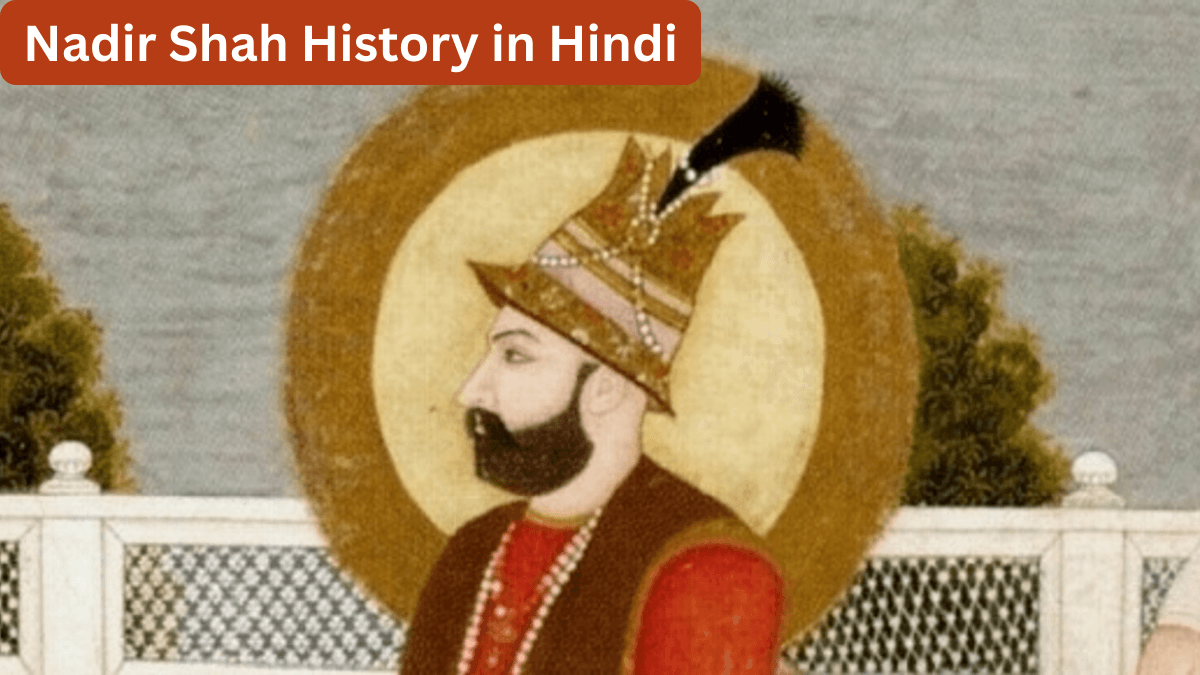Khilji dynasty history: दास वंश या गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया, जिसने 1290 से 1320 ई. तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, मगर इस वंश का साम्राज्य विस्तार और शक्ति वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। खिलजी शासकों ने दास वंश से प्राप्त सिमित साम्राज्य का विस्तार बड़े पैमाने पर किया, जिसमें उत्तर भारत के राजपूत राज्य और दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य शामिल हो गए। यह युग साम्राज्यवाद, सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक नियंत्रण का प्रतीक बना।
खिलजी क्रांति के माध्यम से तुर्की अमीरों के एकाधिकार को नष्ट किया गया और राज्य को धर्म से अलग कर, सम्राट की शक्ति-आधारित बनाया गया। इस लेख में खिलजी वंश की उत्पत्ति, शासकों की उपलब्धियां, नीतियां, विजयें और पतन को विस्तार से समझाया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक स्रोतों जैसे जियाउद्दीन बरनी की ‘तारीख-ए-फिरोजशाही‘, अमीर खुसरो की रचनाओं और अन्य समकालीन वर्णनों का संदर्भ लिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति को विस्तार से समझाया जायेगा।

खिलजी कौन थे? उत्पत्ति और पृष्ठभूमि
सबसे पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि खिलजी सुल्तान आये कहाँ से थे? अधिकांश विद्वान उन्हें तुर्की मूल का मानते हैं, जो अफगानिस्तान के खिलजी क्षेत्र में बस गए थे। फखरुद्दीन और निजामुद्दीन अहमद जैसे इतिहासकार उन्हें तुर्कों की 64 जातियों में से एक बताते हैं। जियाउद्दीन बरनी ने उन्हें तुर्कों से भिन्न बताया, लेकिन अफगान या पठान नहीं माना। खिलजियों ने अफगानिस्तान की हेलमंद नदी क्षेत्र में लंबे समय तक रहकर अफगानों के गुण अपनाए, जैसे साहस और स्वतंत्रता।
गुलाम वंश की नस्लवादी नीतियों से पीड़ित होने के कारण वे विशेषाधिकारविहीन थे। कुछ ऐसिहासिक स्रोतों में जलालुद्दीन खिलजी को चंगेज खान का दामाद बताया जाता है, लेकिन यह विवादास्पद है। भारत आने से पहले वे तुर्किस्तान से थे, जो दिल्ली सल्तनत में सैनिक के रूप में शामिल हुए। खिलजी क्रांति ने तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम किया और सर्वहारा वर्ग को शासन का अवसर दिया। इस क्रांति ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक किया और धर्म के स्थान पर शक्ति को राज्य का आधार बनाया।
खिलजियों का उदय गुलाम वंश के पतन के पश्चात् हुआ, जब शमसुद्दीन कायुमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। ऐतिहासिक रूप से, खिलजी तुर्को-अफगान मूल के थे, और उनका उदय दिल्ली सल्तनत में गैर-तुर्की तत्वों के सशक्तीकरण का प्रतीक था, जैसा कि ब्रिटैनिका एनसाइक्लोपीडिया में वर्णित है। वे मध्य एशिया से आए प्रवासियों के रूप में देखे जाते हैं, जिन्होंने स्थानीय भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
खिलजी क्रांति: साम्राज्य विस्तार का प्रारम्भ
खिलजी क्रांति दिल्ली सल्तनत के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी मोड़ थी। गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान कायुमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन ने इल्बारी तुर्कों का एकाधिकार समाप्त किया। यह क्रांति मात्र राजवंश परिवर्तन नहीं थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। खिलजियों ने सिद्ध किया कि शासन करना विशिष्ट वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। तुर्की अमीरों का प्रभाव कम हुआ और राज्य धर्म (बगदाद के खलीफा से मुक्त) से मुक्त होकर सेक्यूलर बना।
कट्टर उलेमाओं का हस्तक्षेप को नाकारा गया। क्रांति के परिणामस्वरूप सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक हुआ, मंगोल आक्रमण रोके गए और प्रशासन मजबूत हुआ। जलालुद्दीन की उदार नीति और अलाउद्दीन की विजयों ने दिल्ली सल्तनत को बुलंदियों पर पहुँचाया। यह युग इस्लामिक शक्ति के विस्तार और साम्राज्यवाद का प्रतीक बना। क्रांति ने दिल्ली को एशिया की प्रमुख शक्ति बनाया, जहां सैन्य बल और आर्थिक नियंत्रण प्रमुख थे। ऐतिहासिक संदर्भ में, यह क्रांति 1290 ई. में हुई, जब जलालुद्दीन ने किलोखरी में राज्याभिषेक कराया, और यह तुर्की कुलीनों के खिलाफ एक विद्रोह था, जैसा कि विकिपीडिया और अन्य स्रोतों में उल्लिखित है। इसने सल्तनत को अधिक समावेशी बनाया, जिसमें गैर-तुर्की तत्वों को सम्मानजनक स्थान मिला।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी (1290-1296 ई.): उदार शासक की शुरुआत और प्रारंभिक चुनौतियां
जलालुद्दीन खिलजी ने सैनिक से सुल्तान बनने का सफर तय किया। समाना का सूबेदार और कैकुबाद का अंगरक्षक रह चुके जलालुद्दीन ने किलोखरी में राज्याभिषेक कराया, क्योंकि दिल्ली के तुर्क सरदार उसे अफगान मानते थे। धीरे-धीरे उसकी उदारता ने लोगों का दिल जीता। उसने बलबन के रिश्तेदारों को पदों पर बनाए रखा, जैसे मलिक छज्जू को अवध का गवर्नर। हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, लेकिन सिद्दी मौला जैसे विद्रोहियों को दंडित किया। (यह एक विवादस्पद घटना है)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पूरा नाम | जलालुद्दीन फिरोज खिलजी (फिरोज अल-दीन खिलजी) |
| जन्म | लगभग 1220 ई. |
| जन्मस्थान | क़लात, ज़ाबुल प्रांत, अफगानिस्तान |
| पिता का नाम | युग़रुश बेग |
| माता का नाम | अज्ञात |
| शासक कब बना | 1290 ई. (दिल्ली सल्तनत का सुल्तान) |
| पत्नी | अज्ञात (परिवार में बेटियाँ और बेटे थे) |
| संतान | बेटे: अर्कली खाँ, कद्र खाँ, रुक्नुद्दीन इब्राहीम; बेटी: मलिका-ए-जहाँ (अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी) |
| मृत्यु | 22 अक्टूबर 1296 (अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या) |
| उत्तराधिकारी | अलाउद्दीन खिलजी |
मलिक छज्जू का विद्रोह और इसका दमन
1290 ई. में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया और सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ली। जलालुद्दीन ने इसे कुचला और कड़ा-मानिकपुर अलाउद्दीन को सौंपा। ठगों का दमन किया। यह घटना जलालुद्दीन की प्रारंभिक चुनौतियों को दर्शाती है, जहां उसने आंतरिक विद्रोहों को कुशलतापूर्वक कुचला।
आपको यह भी पढ़ना चाहिए-
रणथंबौर अभियान-1291-1292 ई.
दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी (1290-1296 ई.) का रणथंबौर अभियान एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो उसके उदार स्वभाव और सैन्य रणनीति को दर्शाता है। 1290 ई. में गद्दी संभालते ही जलालुद्दीन ने सल्तनत की सीमाओं को मजबूत करने और राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की नीति अपनाई। रणथंबौर का दुर्ग, जो राजस्थान के चौहान वंश के अधीन था, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर स्थित था, चारों ओर गहरी खाइयों और घने जंगलों से घिरा हुआ, जिसे जीतना किसी भी आक्रमणकारी के लिए चुनौतीपूर्ण था। जलालुद्दीन ने इसे जीतकर दिल्ली की दक्षिणी सीमा सुरक्षित करने और राजपूत शक्ति को कुचलने का लक्ष्य रखा।
1291 ई. में सुल्तान ने स्वयं एक बड़ी सेना लेकर रणथंबौर की ओर प्रस्थान किया। सेना में हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी शामिल थे। दुर्ग के शासक हम्मीरदेव चौहान एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने पहले गुलाम वंश के सुल्तानों को भी कठीन चुनौती दी थी। जैसे ही दिल्ली की सेना दुर्ग के निकट पहुंची, राजपूतों ने तीरों और पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। जलालुद्दीन ने दुर्ग को घेराबंदी की रणनीति अपनाई, लेकिन राजपूतों का प्रतिरोध इतना प्रबल था कि मुस्लिम सेना को भारी क्षति हुई। सुल्तान की सेना में बहुत से मुस्लिम सैनिक थे, और दुर्ग पर सीधा आक्रमण करने से हजारों मुस्लिमों की जान जा सकती थी।
जलालुद्दीन, जो स्वयं को एक दयालु मुसलमान मानता था, ने रक्तपात से बचने का निर्णय लिया। वह बोला, “मैं मुस्लिम रक्त नहीं बहाना चाहता।” इस उदारता के कारण अभियान असफल रहा, और सुल्तान बिना दुर्ग जीते वापस लौट आया। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इसे सुल्तान की कमजोरी बताया, लेकिन यह उसकी मानवीय संवेदना का प्रमाण था।
हालांकि, जलालुद्दीन ने हार नहीं मानी। 1292 ई. में उसने पुनः अभियान चलाया, इस बार मंडौर और झाइन पर ध्यान केंद्रित किया। मंडौर (आधुनिक जोधपुर के निकट) और झाइन (राजस्थान में) रणथंबौर के सहयोगी दुर्ग थे। सुल्तान की सेना ने इन पर आक्रमण किया। राजपूत सेनाएं टूट गईं, और दोनों दुर्ग मुस्लिम आक्रांताओं के नियंत्रण में आ गए। मंडौर की विजय से दिल्ली को राजस्थान में मजबूत आधार मिला, और झाइन ने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया।
इन विजयों ने रणथंबौर को अलग-थलग कर दिया, हालांकि मुख्य दुर्ग अभी भी राजपूत हाथों में था। अमीर खुसरो की रचना ‘मिफ्ता-उल-फुतूह’ में इन अभियानों का विस्तृत वर्णन है, जहां सुल्तान को न्यायप्रिय और विजेता बताया गया है। यह अभियान खिलजी वंश की साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत था, जो बाद में अलाउद्दीन ने पूरा किया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार, यह अभियान 1291-1292 ई. के बीच हुआ, और इसमें जलालुद्दीन की उदारता ने उसके सैन्य लक्ष्यों को प्रभावित किया।
मंगोल समस्या
1292 ई. दिल्ली सल्तनत के लिए मंगोल आक्रमण एक निरंतर खतरा थे। चंगेज खान के वंशज हुलागू खान का पौत्र अब्दुल्ला ने लगभग 1.5 लाख मंगोल सैनिकों के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। मंगोल सेना सुनाम तक पहुंच गई, लूटपाट और विनाश करते हुए। जलालुद्दीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी सेना, जिसमें अलाउद्दीन जैसे कुशल सेनापति शामिल थे, ने मंगोलों को लाहौर के निकट रोका। निर्णायक युद्ध में मुस्लिम सेना ने मंगोलों को बुरी तरह हराया। हजारों मंगोल मारे गए, और अब्दुल्ला भाग निकला।
विजय के बाद जलालुद्दीन की उदारता फिर सामने आई। मंगोलों से समझौता किया, और उन्हें वापस लौटने दिया। चंगेज खान के एक वंशज उलगू खान ने अपने 4,000 साथियों सहित इस्लाम धर्म स्वीकार किया। सुल्तान ने उलगू से अपनी पुत्री का विवाह किया और दिल्ली के निकट ‘मुगलपुर‘ नामक बस्ती बसाई। इन नव-मुस्लिमों को ‘नए मुसलमान‘ कहा गया। शुरू में यह कदम सराहनीय लगा, क्योंकि इससे मंगोल खतरा कुछ समय के लिए कम हुआ। लेकिन बाद में ये नए मुसलमान दिल्ली सरकार के लिए उत्पाती साबित हुए। वे विद्रोह करते, लूटपाट करते और सत्ता के लिए षड्यंत्र रचते।
अलाउद्दीन को बाद में इनका दमन करना पड़ा। बरनी ने इसे जलालुद्दीन की ‘अनुचित छूट’ बताया, जो सल्तनत के लिए संकट का कारण बनी। यह घटना दिल्ली की उत्तर-पश्चिमी सीमा की रक्षा की जटिलता दर्शाती है। मंगोल आक्रमणों की यह श्रृंखला 1292 ई. में चरम पर थी, और जलालुद्दीन की नीति ने बाद के शासकों के लिए समस्याएं उत्पन्न कीं।
दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण
जलालुद्दीन के शासन में दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जो सल्तनत के विस्तार का प्रारंभिक कदम था। 1292 ई. में अलाउद्दीन, जो कड़ा–मानिकपुर का सूबेदार था, ने चाचा की अनुमति लेकर मालवा, भिलसा और देवगिरि पर अभियान किया। देवगिरि (आधुनिक दौलताबाद, महाराष्ट्र) यादव वंश के रामचंद्रदेव का राज्य था, जो अपार धन-संपत्ति से समृद्ध था। अलाउद्दीन ने गुप्त रूप से सेना लेकर विंध्य पर्वत पार किया। रामचंद्रदेव अप्रत्याशित आक्रमण से घबरा गए; उनका पुत्र शंकरदेव सेना लेकर दक्षिण गया हुआ था।
अलाउद्दीन की सेना ने देवगिरि को घेर लिया। राजपूतों ने प्रतिरोध किया, लेकिन हार गए। रामचंद्रदेव ने संधि की और भारी फिरौती दी: सोना, चांदी, मोती, रेशम और हाथी। अलाउद्दीन लूट का सामान लेकर कड़ा लौटा। शंकरदेव लौटकर लड़ने आया, लेकिन फिर हार गया। यह लूट इतनी विशाल थी कि अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। उसने सोचा, दिल्ली का सिंहासन अब उसका है।
यह अभियान दक्षिण पर पहला मुस्लिम हमला था, जिसने विंध्य के पार विजय का द्वार खोला। दक्कन की आर्थिक क्षति हुई, लेकिन दिल्ली को धन मिला। जलालुद्दीन की उदारता ने सरदारों में षड्यंत्र बढ़ाए; वे अलाउद्दीन की सफलता से ईर्ष्यालु थे।
अमीर खुसरो ने ‘मिफ्ता-उल-फुतूह‘ में इसे वीरतापूर्ण बताया। सुल्तान ने कहा, “मैं वृद्ध मुसलमान हूं, रक्त बहाना पसंद नहीं,” लेकिन 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन ने कड़ा में उसकी हत्या कर दी। अलमास बेग ने छुरा घोंपा, और अलाउद्दीन सुल्तान बना। यह घटना खिलजी वंश के आंतरिक संघर्षों को उजागर करती है।
अलाउद्दीन खिलजी का उत्कर्ष: शासनकाल: 1296-1316 ई.
अलाउद्दीन खिलजी (शासनकाल: 1296-1316 ई.) दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। वह संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। सुल्तान बनने से पहले उसे इलाहाबाद के पास कड़ा की जागीर मिली हुई थी। उसका बचपन का नाम अली गुरशास्प था। दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने के बाद उसे ‘अमीर-ए-तुजुक‘ का पद प्राप्त हुआ।
मलिक छज्जू के विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा-मनिकपुर की सूबेदारी सौंपी। भिलसा, चंदेरी और देवगिरि अभियानों से हासिल हुई अपार संपत्ति ने उसकी स्थिति को और मजबूत बनाया। इस शक्ति के शिखर पर पहुंचकर अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 22 अक्टूबर 1296 को करवा दी और दिल्ली के बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया।

| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पूरा नाम | अलाउद्दीन खिलजी (जन्म नाम: अली गुरशास्प) |
| उपाधि | अमीर-ए-तुजुक, सिकंदर सानी, यामिन-उल-खिलाफत-नासिरी-अमीर-उल-मोमिनीन |
| जन्म | लगभग 1266-1267 ई. |
| जन्मस्थान | क़लात, ज़ाबुल प्रांत, अफगानिस्तान |
| पिता का नाम | शिहाबुद्दीन मसूद (जलालुद्दीन खिलजी का भाई) |
| माता का नाम | अज्ञात |
| शासक कब बना | 1296 ई. (दिल्ली सल्तनत का सुल्तान) |
| पत्नी | मलिका-ए-जहाँ (जलालुद्दीन की बेटी), महरू (अल्प खाँ की बहन), कमला देवी (गुजरात की रानी), झटयापली (देवगिरि की राजकुमारी) |
| संतान | बेटे: खिज्र खाँ, शादी खाँ, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, शिहाबुद्दीन उमर |
| मृत्यु | 4 जनवरी 1316 ई. (बीमारी से) |
| मृत्यु का कारण | जलोदर रोग |
| उत्तराधिकारी | शिहाबुद्दीन उमर (नाममात्र), फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह |
अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था
राज्याभिषेक के बाद पैदा हुई चुनौतियों का कुशलतापूर्वक मुकाबला करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन प्रणाली का अनुशरण किया, जिसके तहत उसने राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू किया। अपनी प्रारम्भिक विजयों से उत्साहित होकर उसने ‘सिकंदर सानी‘ की उपाधि अपनाई और इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया।
विश्व विजय और एक नया धर्म स्थापित करने की योजना को दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया। हालांकि उसने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते हुए ‘यामिन-उल-खिलाफत-नासिरी-अमीर-उल-मोमिनीन‘ की उपाधि ली, लेकिन खलीफा से पद की औपचारिक स्वीकृति नहीं ली। उलेमा वर्ग को शासन में दखल नहीं देने दिया। इस्लामी सिद्धांतों की बजाय राज्य हित को सर्वोच्च महत्व दिया। अलाउद्दीन के काल में निरंकुशता चरम पर पहुंच गई; उसने न इस्लाम के नियमों का सहारा लिया और न उलेमा की राय मानी। इस तरह उसने सत्ता को धर्म की बजाय सुल्तान की शक्ति से चलाया।
विद्रोहों का दमन
पहला विद्रोह-अलाउद्दीन के शासन में कई विद्रोह हुए, जिन्हें कुचल दिया गया। 1299 ई. में गुजरात अभियान की लूट के बंटवारे पर ‘नए मुसलमानों (पूर्व मंगोलियन)’ का विद्रोह नुसरत खान ने दबाया।
दूसरा विद्रोह– सुल्तान के भतीजे अकत खान ने मंगोल मुसलमानों की मदद से किया, जिसमें सुल्तान पर घातक हमला हुआ; अकत खान को पकड़कर मार डाला गया।
तीसरा विद्रोह- सुल्तान की बहन के पुत्र मलिक उमर और मंगू खान ने किया, लेकिन दोनों को हराकर हत्या कर दी गई।
चौथा विद्रोह- दिल्ली के हाजी मौला ने किया, जिसे हमीदुद्दीन ने कुचला। तुर्क अमीरों के विद्रोहों के कारणों का विश्लेषण कर अलाउद्दीन ने चार अध्यादेश जारी किए:
- अमीरों को दी गई दान, उपहार और पेंशन की भूमि जब्त कर उन पर भारी कर लगाया, जिससे उनकी आर्थिक शक्ति कम हुई।
- गुप्तचर विभाग को मजबूत बनाया; ‘बरीद‘ (संदेशवाहक) और ‘मुनहिन‘ (जासूस) नियुक्त किए।
- शराब, भांग और जुआ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया।
- अमीरों के पारस्परिक मेल-जोल, सार्वजनिक आयोजनों और वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाई।
ये अध्यादेश पूरी तरह सफल रहे। हिंदू लगान अधिकारियों जैसे खूत, मुकदमों के विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार
अलाउद्दीन साम्राज्यवादी सुल्तान था। उसने उत्तर भारत के राज्यों पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, जबकि दक्षिण से वार्षिक कर वसूला।
गुजरात विजय (1298 ई.): उलुग खान और नुसरत खान को भेजा। अहमदाबाद के पास बघेल राजा कर्ण (राजकरन) को पराजित। कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरि भाग गया। अलाउद्दीन ने कर्ण की संपत्ति और पत्नी कमला देवी को दिल्ली लाया, बाद में कमला देवी से विवाह किया और उसे प्रिय रानी बनाया। नुसरत खान ने हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा। सेना ने सूरत, सोमनाथ और कैंबे तक लूटा।
जैसलमेर विजय (1299 ई.): घोड़ों की चोरी पर शासक दूदा और तिलक सिंह को हराया।
रणथंबौर विजय (जुलाई 1301 ई.): शासक हम्मीरदेव ने मंगोल विद्रोहियों मुहम्मद शाह और केहब को शरण दी थी। अलाउद्दीन ने किला जीता; हम्मीरदेव मारा गया। विश्वासघाती रणमल और साथियों का वध। ‘तारीख-ए-अलाई‘ और ‘हम्मीर महाकाव्य‘ में जौहर का वर्णन। नुसरत खान की मौत हुई।
चित्तौड़ विजय (28 जनवरी 1303 ई.): मेवाड़ के राणा रतन सिंह की राजधानी। कुछ स्रोतों में रानी पद्मिनी की सुंदरता को कारण बताया, लेकिन अमीर खुसरो में रानी शैबा-सुलेमान प्रेम का उल्लेख। किला जीता; रतन सिंह शहीद, पद्मिनी सहित महिलाओं ने जौहर किया। 30,000 राजपूत मारे गए। चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद रखा, खिज्र खान को सौंपा। बाद में मालदेव को दिया। अलाउद्दीन की मौत 1321 ई. के बाद हम्मीरदेव (गुहिलोत) ने चित्तौड़ मुक्त कराया।
मालवा विजय (1305 ई.): महलकदेव और सेनापति हरनंद (कोका प्रधान) मारे गए। आईन-उल-मुल्क के नेतृत्व में उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी जीते।
सिवाना (1308 ई.): परमार शासक शीतलदेव मारा गया; कमालुद्दीन गुर्ग नियुक्त।
जालौर: कान्हणदेव ने 1304 ई. में अधीनता स्वीकार की, लेकिन बाद में स्वतंत्र हुआ। 1305 ई. में कमालुद्दीन गुर्ग ने हराकर हत्या की। 1311 ई. तक उत्तर भारत में नेपाल, कश्मीर, असम को छोड़ शेष जीता।
अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय अभियान
अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316 ई.) दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी सुल्तान था, जिसने अपनी सैन्य शक्ति से उत्तर भारत को मजबूत करने के बाद दक्षिण की ओर रुख किया। उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राज्यों से अपार धन लूटना और उन पर वार्षिक कर (ट्रिब्यूट) थोपना था, ताकि मंगोल आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए मजबूत सेना खड़ी की जा सके। दक्षिण में उस समय तीन प्रमुख हिंदू राज्य शक्तिशाली थे:
- यादव वंश (देवगिरि, आज का औरंगाबाद क्षेत्र),
- काकतीय वंश (तेलंगाना, राजधानी वारंगल),
- होयसल वंश (द्वारसमुद्र, आज का हलेबीदु)।
इन अभियानों का नेतृत्व किया मलिक काफूर ने, जो अलाउद्दीन का विश्वस्त सेनापति और एक हिजड़ा (खोजा) था। मूल रूप से गुजरात का एक हिंदू गुलाम (ख्वाजा सरा), काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दीनार में खरीदा था। उसकी वफादारी, बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल ने उसे ‘हजार दिनारी’ की उपाधि दिलाई। काफूर ने इन अभियानों में न केवल विजय प्राप्त की, बल्कि दिल्ली के लिए अनगिनत हाथी, घोड़े, रत्न और सोना लूटकर लाया।
1. देवगिरि पर आक्रमण (1307-1308 ई.)
देवगिरि के यादव शासक रामचंद्र देव ने पहले अलाउद्दीन को कर देना स्वीकार किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया। इससे क्रुद्ध होकर अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को 1307 में दक्षिण भेजा।
- यात्रा का रोचक प्रसंग: रास्ते में काफूर ने बघेल राजा कर्ण देव की पुत्री देवल देवी को पकड़ा और दिल्ली भेज दिया। देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान से हुआ, जो एक राजनीतिक गठबंधन था।
- विजय: काफूर की सेना ने देवगिरि को घेर लिया। रामचंद्र ने युद्ध के बजाय आत्मसमर्पण किया। लूट में अपार सोना-चांदी, 600 हाथी और अनगिनत रत्न मिले।
- उदारता का प्रदर्शन: अलाउद्दीन ने रामचंद्र को मारने के बजाय सम्मान दिया। उसे ‘राय रायान’ की उपाधि, नवसारी (गुजरात) में जागीर और 1 लाख टके वार्षिक पेंशन दी। रामचंद्र दिल्ली आया, जहां अलाउद्दीन ने उसे अपना मित्र बनाया। बाद में रामचंद्र ने अन्य दक्षिणी अभियानों में दिल्ली की मदद की। यह नीति अलाउद्दीन की दूरदर्शिता दिखाती है – विजय के बाद दोस्ती से स्थायी नियंत्रण।
2. वारंगल (काकतीय) पर आक्रमण (1309-1310 ई.)
अगला लक्ष्य था काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव की राजधानी वारंगल। रामचंद्र देव की मदद से काफूर की सेना तेलंगाना पहुंची। वारंगल एक मजबूत किले वाला शहर था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था।
- घेराबंदी और समर्पण: महीनों की लड़ाई के बाद प्रताप रुद्रदेव ने हार मान ली। उसने समर्पण के रूप में सोने की एक विशाल मूर्ति (खुद की प्रतिमा) को जंजीरों से बांधकर भेजी – यह अपमानजनक लेकिन प्रतीकात्मक था।
- लूट और कर: दिल्ली को 100 हाथी, 700 घोड़े, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और अपार धन मिला। प्रताप रुद्रदेव ने वार्षिक कर स्वीकार किया। कोहिनूर हीरा बाद में विश्व प्रसिद्ध हुआ, जो आज ब्रिटिश ताज में जड़ा है।
- महत्व: यह अभियान दक्षिण में दिल्ली की पहुंच को मजबूत बनाया और काकतीयों को कमजोर किया।
3. द्वारसमुद्र (होयसल) पर आक्रमण (1311 ई.)
होयसल शासक वीर बल्लाल III की राजधानी द्वारसमुद्र अगला निशाना थी। होयसल मंदिरों और कला के लिए प्रसिद्ध थे।
- आत्मसमर्पण: बल्लाल III ने युद्ध टाला और काफूर के सामने झुका। उसने राजकीय मुकुट, छत्र, खिताब और 10 लाख टके भेंट किए।
- सहयोग: बल्लाल ने माबर (पांड्य) अभियान में दिल्ली की मदद की। अलाउद्दीन ने उसे भी सम्मानित रखा, जिससे होयसल दिल्ली के अधीन हो गए।
- सांस्कृतिक प्रभाव: होयसल मंदिरों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कर थोपकर आर्थिक नियंत्रण स्थापित हुआ।
4. माबर (पांड्य) अभियान (1311 ई.)
सबसे दक्षिणी और धनवान अभियान। पांड्य राज्य (आज का तमिलनाडु) में सुंदर पांड्य और वीर पांड्य भाइयों में गद्दी का झगड़ा था। सुंदर पांड्य ने दिल्ली से मदद मांगी।
- विजय मार्ग: काफूर ने होयसल की मदद से माबर पहुंचा। वीरधवल (वीर पांड्य का किला) जीता। रास्ते में बरमतपती के लिंग महादेव मंदिर को लूटा।
- रामेश्वरम तक: काफूर सबसे दक्षिण तक पहुंचा। रामेश्वरम मंदिर तोड़ा और उसकी जगह मस्जिद बनवाई – यह धार्मिक असहिष्णुता का उदाहरण था।
- लूट: सबसे अधिक धन – हजारों हाथी, घोड़े, रत्न और सोना। लेकिन वीर पांड्य भाग निकला, इसलिए पूर्ण विजय नहीं हुई।
- महत्व: यह अभियान दिल्ली की सेना को हिंद महासागर तक ले गया, लेकिन लौटते समय बीमारी और थकान से कई सैनिक मरे।
ये अभियान अलाउद्दीन की सैन्य genius दिखाते हैं। मलिक काफूर ने मात्र 4 वर्षों में दक्षिण को लूटकर दिल्ली को विश्व की सबसे धनी राजधानी बनाया। धन से अलाउद्दीन ने स्थायी सेना, बाजार नियंत्रण और मंगोल प्रतिरोध मजबूत किया। हालांकि, ये लूटें थीं न कि स्थायी साम्राज्य विस्तार – अलाउद्दीन की मृत्यु (1316) के बाद दक्षिणी राज्य फिर स्वतंत्र हो गए। फिर भी, ये भारत के मध्यकालीन इतिहास में इस्लामी आक्रमणों की चरम सीमा थे, जिन्होंने दक्षिणी संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। काफूर की कहानी एक गुलाम से सेनापति बनने की प्रेरणा है, लेकिन लूट और मंदिर विनाश नैतिक सवाल उठाते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल आक्रमण
अलाउद्दीन खिलजी (शासनकाल: 1296-1316 ई.) दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक था। उसके समय में मंगोल (चंगेज खान के वंशज) उत्तर-पश्चिम से बार-बार आक्रमण करते थे। ये आक्रमण विनाशकारी थे – गांव जलाते, हत्या करतेऔर लूटते। 1296 से 1308 तक कम से कम 6 बड़े मंगोल आक्रमण हुए, जिनमें अब्दुल्ला, कदर खान, सल्दी जैसे सेनापति शामिल थे। मंगोलों की ताकत: तेज घुड़सवार, धनुष-बाण और आश्चर्यजनक हमले।
अलाउद्दीन ने जफर खान, उलुग खान, मलिक काफूर और गाजी मलिक (बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक) जैसे सेनापतियों की मदद से इन्हें रोका। नीचे प्रत्येक आक्रमण का विस्तृत वर्णन – पृष्ठभूमि, युद्ध, परिणाम और महत्व:
1. 1297-98 ई.: कादर खान का पंजाब आक्रमण
- पृष्ठभूमि: अलाउद्दीन ने刚刚 सत्ता हथियाई थी (1296)। मंगोल सरदार कादर खान ने 20,000-30,000 सैनिकों के साथ पंजाब पर हमला किया। उद्देश्य: लूट और दिल्ली को कमजोर करना।
- युद्ध: अलाउद्दीन ने अपने भाई उलुग खान और सेनापति जफर खान को भेजा। जालंधर के पास निर्णायक युद्ध हुआ।
- दिल्ली की सेना ने मंगोलों को घेर लिया। जफर खान की बहादुरी से मंगोलों की घुड़सवार टुकड़ी टूट गई।
- मंगोलों ने भारी नुकसान उठाया; कादर खान भाग निकला।
- परिणाम: कादर खान की हार। हजारों मंगोल मारे गए, लूट का माल वापस छीना। दिल्ली की पहली बड़ी जीत।
- महत्व: अलाउद्दीन की सेना की ताकत साबित हुई। इसने मंगोलों को सतर्क किया कि दिल्ली अब कमजोर नहीं।
2. 1298 ई.: सलदी का सिवान आक्रमण
- पृष्ठभूमि: कादर की हार से क्रुद्ध होकर सलदी ने सिवान (सियालकोट क्षेत्र) पर हमला किया। सेना: लगभग 10,000 घुड़सवार।
- युद्ध: जफर खान फिर मैदान में। सिवान के मैदान में मंगोलों को रोका।
- जफर खान ने रात में आश्चर्यजनक हमला किया। मंगोलों की सप्लाई लाइन काटी।
- हाथों-हाथ लड़ाई में मंगोल धनुष व्यर्थ साबित हुए।
- परिणाम: सलदी हारकर भागा। दिल्ली ने क्षेत्र पर फिर नियंत्रण स्थापित किया।
- महत्व: लगातार दूसरी जीत। अलाउद्दीन ने पंजाब में स्थायी चौकियां बनानी शुरू कीं।
3. 1299 ई.: कुतलुग ख्वाजा का दिल्ली तक आक्रमण
- पृष्ठभूमि: सबसे खतरनाक आक्रमण। कुतलुग ख्वाजा (चंगेज खान का वंशज) ने 50,000+ सैनिकों के साथ दिल्ली पर सीधा हमला किया। अलाउद्दीन व्यस्त था (गुजरात अभियान)।
- युद्ध: जफर खान और उलुग खान को दिल्ली की रक्षा सौंपी। किली (दिल्ली के पास) युद्ध।
- मंगोल दिल्ली के द्वार तक पहुंचे। जफर खान ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन अलाउद्दीन से समय पर सहायता नहीं मिली (संदेह या देरी के कारण)।
- जफर खान वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मौत से सेना में अफरा-तफरी।
- परिणाम: मंगोल लूटकर भागे, लेकिन दिल्ली बची। जफर खान की मौत बड़ा नुकसान।
- महत्व: अलाउद्दीन को सबक मिला – सेना में विश्वासघात रोकने के लिए सुधार शुरू। जफर खान को ‘शहीद’ माना गया।
4. 1303 ई.: तारगी का सीरी घेरा
- पृष्ठभूमि: तारगी (मंगोल सेनापति) ने 1 लाख+ सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला। अलाउद्दीन ने नया किला सीरी बनवाया था।
- युद्ध: 2 महीने की घेराबंदी।
- मंगोलों ने सीरी को चारों ओर से घेरा। तोपें और पत्थर फेंके।
- अलाउद्दीन किले में रहा, जासूसों से मंगोल शिविर की खबर ली। रात में जवाबी हमले।
- अनाज की कमी से मंगोल थके। अलाउद्दीन ने सोने की मुहरें फेंककर मंगोलों को लालच दिया (विखंडन नीति)।
- परिणाम: तारगी लूटकर भागा, लेकिन 30,000 मंगोल मारे। दिल्ली की सबसे बड़ी रक्षात्मक जीत।
- महत्व: अलाउद्दीन को ‘दूसरा सिकंदर’ कहा गया। इसने स्थायी सेना बनाने की प्रेरणा दी।
5. 1305 ई.: अलीबेग, तार्ताक और तारगी का अमरोहा आक्रमण
- पृष्ठभूमि: तीन मंगोल सेनापति (अलीबेग, तार्ताक, तारगी) ने 50,000 सैनिकों के साथ अमरोहा (उत्तर प्रदेश) पर हमला।
- युद्ध: अलाउद्दीन ने मलिक काफूर (दक्षिण विजेता) और गाजी मलिक (तुगलक) को भेजा।
- अमरोहा का मैदान: दिल्ली की सेना ने मंगोलों को घेरा। घुड़सवार टक्कर में मंगोल हारे।
- काफूर की चालाकी: नकली पीछे हटना, फिर पलटकर हमला।
- परिणाम: मंगोल सेनापतियों को पकड़ा। दिल्ली में हाथी पर परेड कराया, फिर मार डाला। हजारों कैदी।
- महत्व: मंगोलों की कमर टूटீ। गाजी मलिक की प्रसिद्धि बढ़ी (बाद में सुल्तान बना)।
6. 1306 ई.: इकबालमंद का रावी नदी आक्रमण
- पृष्ठभूमि: अंतिम बड़ा आक्रमण। इकबालमंद ने रावी नदी पार कर पंजाब लूटा।
- युद्ध: गाजी मलिक अकेले मैदान में।
- रावी तट: मंगोलों को नदी पार करने नहीं दिया। तीरों की बौछार और घुड़सवार हमला।
- इकबालमंद की सेना डूबी या मारी गई।
- परिणाम: पूर्ण हार। मंगोल भागे, फिर कभी बड़े हमले नहीं किए।
- महत्व: 1306 के बाद मंगोल आक्रमण रुक गए। अलाउद्दीन की सीमा मजबूत हुई।
गाजी मलिक को सीमा रक्षक बनाया। 1304 ई. में सीरी राजधानी बनाई, किलेबंदी की।
अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों को स्थायी समस्या माना और व्यवस्थित सुधारों से निपटा। उसकी रणनीति: मजबूत सेना, किले, जासूसी और आर्थिक नियंत्रण।
1. सीमाओं की मजबूती और किलों का निर्माण
- उत्तर-पश्चिम सीमा (सिंधु नदी से दिल्ली तक) पर मजबूत दुर्ग बनवाए: सिरी, कैथल, अमरोहा आदि।
- पुराने किलों को मजबूत किया। दोहरी दीवारें (बाहरी और भीतरी) बनवाईं, जिनमें खाई, कांटेदार झाड़ियां और तोपें लगीं।
- स्थायी चौकियां: हर 10-20 किमी पर सैनिक टुकड़ियां तैनात। मंगोलों को दिल्ली तक पहुंचने नहीं दिया।
2. विश्व की सबसे मजबूत स्थायी सेना का गठन
- पहले का सिस्टम: जागीरदारों की सेना – जरूरत पर बुलाते, लेकिन अविश्वसनीय।
- अलाउद्दीन का सुधार: नकद वेतन पर स्थायी सेना (लगभग 4-5 लाख सैनिक)।
- घुड़सवार: 50-60 टंका महीना।
- पैदल: 20-30 टंका।
- घोड़ों की ब्रांडिंग (दाग): हर घोड़े पर राजकीय चिह्न – काला बाजार रोका।
- सैनिकों का वर्णनात्मक रोल (हुलिया): चेहरा, कद दर्ज – भगोड़े पकड़े जाते।
- परिणाम: सेना हमेशा तैयार। 1303 में जैत्राण (चित्तौड़) के मंगोल आक्रमण को हराया।
3. जासूसी और खुफिया तंत्र
- बारिद (जासूस) नेटवर्क: मंगोल शिविरों में घुसपैठ।
- आक्रमण की खबर महीनों पहले मिलती। अलाउद्दीन को ‘दूसरा सिकंदर’ कहा गया क्योंकि वह पहले हमला करता।
- राजनीतिक चाल: मंगोल सरदारों को रिश्वत देकर बांटा। कुछ को दिल्ली में नौकरी दी।
4. आर्थिक सुधार: धन का स्रोत
- मंगोलों से लड़ने के लिए अपार धन चाहिए था।
- दक्षिण विजय (मलिक काफूर के अभियान): देवगिरि, वारंगल, होयसल से लाखों टंका, हाथी, कोहिनूर लूटा।
- कर सुधार:
- खराज (भूमि कर) 50% तक।
- लेकिन किसानों को राहत: सूखा में माफ।
- बाजार नियंत्रण: सस्ते अनाज, कपड़े – सेना को सस्ता रसद।
- शाहना-ए-मंडी: बाजार निरीक्षक – कालाबाजारी पर सजा।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति सुल्तान के पास। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि माना; उलेमा से अलग रहा। प्रांतों पर कड़ा नियंत्रण।
मंत्री:
- दीवान-ए-वजारत: वजीर (ख्वाजा खातिर, नुसरत खान आदि); वित्त, सेना नेतृत्व।
- दीवान-ए-आरिज: युद्धमंत्री (मलिक नासिरुद्दीन); भर्ती, वेतन, साज-सज्जा।
- दीवान-ए-इंशा: दबीर-ए-खास; राजकीय लेखक, उद्घोषणा।
- दीवान-ए-रसालत: विदेश, कूटनीति।
- दीवान-ए-रियासत: आर्थिक नियंत्रण (नया विभाग बनाया)।
नए विभाग: दीवान-ए-मुस्तखराज (बकाया वसूली), दीवान-ए-रियासत।
बाजार पद: शहना-ए-मंडी (दरोगा), मुहतसिब (माप-तौल)। अन्य: वकील-ए-दर (महल की देखभाल करने वाला), सरजानदार (अंगरक्षक), अमीर-ए-आखूर (घुड़साल का अधिकारी) आदि।
न्याय: सुल्तान उच्चतम; सद्र-ए-जहां, काजी-उल-कुजात, नायब काजी, मुफ्ती। अमीर-ए-दाद प्रभावशाली मामलों के लिए।
पुलिस-गुप्तचर: कोतवाल प्रमुख; दीवान-ए-रियासत व्यापार नियंत्रण। शहना, दंडाधिकारी। मुहतसिब (आचार रक्षक)। बरीद-ए-मुमालिक प्रमुख; बरीद, मुनही जासूस।
डाक: घुड़सवार, लिपिक; त्वरित सूचना।
सैन्य: 4.75 लाख सैनिक (फरिश्ता)। घोड़ों का दाग, हुलिया। नकद वेतन: एक अस्पा 234 टंका, दो अस्पा 378 टंका। तुमन (10,000)। घुड़सवार प्रमुख।
आर्थिक सुधार
विशाल सेना और 50,000 दासों के खर्च के लिए। बरनी: मंगोल मुकाबला। खुसरो: जनकल्याण। दिल्ली तक सीमित (मोरलैंड, लाल) या पूरे में (सक्सेना)।
मूल्य नियंत्रण:
- गेहूं: 7.5 जीतल/मन, चावल: 5, जौ: 4, उड़द: 5, घी: 1 जीतल/2.5 किलो।
- शहना-ए-मंडी: अनाज बाजार; मलिक कबूल।
- सराय-ए-अदल: कपड़ा आदि; बदायूं गेट; 1-10,000 टंका।
- पशु बाजार: घोड़ा 10-120 टंका; दलाली प्रतिबंध।
क्रियान्वयन: लगान अनाज में (दोआब), आधा अनाज-आधा नकद (झाइन)। राशन कार्ड; आधा मन/व्यक्ति। गोदाम अकाल के लिए। व्यापारी पंजीकरण, जमानत।
अधिकारी: दीवान-ए-रियासत (मलिक याकूब); शहना-ए-मंडी, बरीद, मुनहियान। मुहतसिब, नाजिर।
दंड: कालाबाजारी पर कोड़े, मांस काटना, जब्ती।
राजस्व: मिल्क, इनाम, वक्फ भूमि खालसा में। खूत-मुकदम विशेषाधिकार समाप्त। 50% खराज; मसाहत पर। विस्वा इकाई। चराई, चरी कर नए। जजिया (गैर-मुस्लिम), खुम्स (लूट का 4/5 राज्य), जकात (मुस्लिम)। दीवान-ए-मुस्तखराज बकाया वसूली। शर्फ कायिनी को श्रेय।
मृत्यु और निर्माण
जलोदर से 5 जनवरी 1316 ई. को मृत्यु। दरबार में अमीर खुसरो, हसन निजामी को संरक्षण। अलाई दरवाजा (वृत्ताकार), कुश्क-ए-शिकार बनवाया; प्रारंभिक तुर्की कला का उत्कृष्ट नमूना।

अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद का इतिहास
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ई. को जलोदर रोग (एडिमा) से हुई। उसकी मौत के समय उसका सबसे छोटा पुत्र और घोषित उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर केवल 6 वर्ष का था। अलाउद्दीन का विश्वसनीय सेनापति और गुलाम मलिक काफूर (हजारदिनारी) ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने अलाउद्दीन के बड़े पुत्रों खिज्र खान और शादी खान की आंखें फोड़ दीं और उन्हें ग्वालियर किले में कैद कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह (अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र) को नाममात्र का सुल्तान बनाया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति मलिक काफूर के हाथ में रही। यह अवधि दिल्ली सल्तनत में अस्थिरता और षड्यंत्रों की शुरुआत थी।
मलिक काफूर का अल्पकालिक शासन (जनवरी 1316 – फरवरी 1316)
- मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की मृत्यु को कुछ दिनों तक गुप्त रखा ताकि सत्ता स्थिर कर सके।
- उसने मुबारक शाह को सुल्तान घोषित किया और खुद को नायब-ए-मुल्क (उप-शासक) बनाया।
- काफूर की क्रूरता और हिंदू मूल (वह गुजरात से खरीदा गया गुलाम था) के कारण दरबारी अमीरों में असंतोष बढ़ा।
- फरवरी 1316 में अमीरों ने षड्यंत्र रचा और काफूर की हत्या कर दी। मुबारक शाह को पूर्ण सुल्तान बना दिया गया।
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का शासन (1316-1320 ई.)
- मुबारक शाह ने सत्ता संभालते ही अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को उलट दिया:
- आर्थिक सुधार समाप्त: बाजार नियंत्रण, मूल्य निर्धारण और राशनिंग प्रणाली खत्म कर दी। इससे महंगाई बढ़ी लेकिन व्यापारियों को राहत मिली।
- उदार नीतियां: कैदियों को रिहा किया, जब्त भूमियां लौटाईं, करों में छूट दी।
- सैन्य कमजोरी: स्थायी सेना को भंग कर वेतन बढ़ाया, लेकिन अनुशासन ढीला पड़ा।
- मुबारक शाह ने खुद को ‘खलीफतुल्लाह’ (ईश्वर का खलीफा) घोषित किया और सिक्कों पर यह उपाधि अंकित कराई।
- विजय अभियान:
- देवगिरि (1317 ई.): यादव शासक हरपाल देव ने कर रोक दिया; मुबारक ने अभियान भेजा, हरपाल को कैद कर फांसी दी। देवगिरि को दिल्ली में मिला लिया।
- वारंगल (1318 ई.): काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने विद्रोह किया; मुबारक की सेना ने वारंगल जीता, प्रताप रुद्रदेव को कैद कर दिल्ली लाया और इस्लाम कबूल करवाया।
- मुबारक शाह विलासिता में डूब गया। उसका प्रिय पति खुसरो खान (एक हिंदू परिवर्तित, मूल नाम हसन) को उच्च पद दिए।
- पतन: खुसरो खान ने मुबारक शाह की हत्या (अप्रैल 1320 ई.) कर खुद सुल्तान बना (नासिरुद्दीन खुसरो शाह)। उसने इस्लाम त्याग हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू सरदारों को पद दिए। इससे मुस्लिम अमीर भड़क उठे।
खिलजी वंश का अंत और तुगलक वंश की स्थापना (1320 ई.)
- खुसरो शाह का शासन केवल 4 महीने चला। उसकी हिंदू-समर्थक नीतियों से असंतोष बढ़ा।
- पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक (गियासुद्दीन तुगलक) ने विद्रोह किया। उसने दिल्ली पर चढ़ाई की, खुसरो शाह को हराया और उसकी हत्या कर दी (सितंबर 1320 ई.)।
- गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। वह अलाउद्दीन के समय का सीमा रक्षक था, जिसने मंगोल आक्रमण रोके थे।
- तुगलक वंश (1320-1414 ई.) ने सल्तनत को पुनर्जीवित किया। गियासुद्दीन ने देवगिरि, वारंगल को फिर अधीन किया और प्रशासन सुधारा।
प्रभाव और परिणाम
- खिलजी वंश का अंत: 1290 से 1320 तक चला यह वंश केवल 30 वर्षों में समाप्त हुआ। आंतरिक कलह, कमजोर उत्तराधिकारी और गुलामों की साजिशें मुख्य कारण।
- सल्तनत पर प्रभाव: अलाउद्दीन की विजयें (दक्षिण तक विस्तार) बनी रहीं, लेकिन आर्थिक नीतियां ढीली पड़ने से राजकोष कमजोर हुआ।
- सामाजिक परिवर्तन: मुबारक और खुसरो के समय धार्मिक उदारता बढ़ी, लेकिन मुस्लिम रूढ़िवादियों का विरोध।
- इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी (‘तारीख-ए-फिरोजशाही’) ने इस काल को अराजकता का दौर बताया, जबकि अमीर खुसरो ने मुबारक की उदारता की प्रशंसा की।
यह अवधि दिल्ली सल्तनत के लिए संक्रमण काल थी, जो तुगलक वंश की मजबूती का आधार बनी। मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने आगे साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। (शब्द संख्या: 812)
अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का विस्तार से मूल्यांकन
दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी (शासनकाल: 1296-1316 ई.) को एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी अर्थशास्त्री के रूप में याद किया जाता है। उसकी बाजार नियंत्रण नीतियाँ (Market Control Policies) सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम थीं, जो मध्यकालीन भारत में मूल्य नियंत्रण, राशनिंग और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की पहली व्यवस्थित मिसाल थीं।
ये नीतियाँ केवल दिल्ली शहर तक सीमित थीं (कुछ इतिहासकारों के अनुसार पूरी सल्तनत में), और इनका मुख्य उद्देश्य एक विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर बनाए रखना था, ताकि मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया जा सके और साम्राज्य का विस्तार हो सके।
समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी की ‘तारीख-ए-फिरोजशाही‘, अमीर खुसरो की ‘खजाइन-उल-फुतूह‘ और फरिश्ता की रचनाओं से इन नीतियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। आइए, इन नीतियों के उद्देश्य, क्रियान्वयन, बाजारों के प्रकार, अधिकारियों की भूमिका, दंड व्यवस्था और प्रभावों को विस्तार से समझें।
नीतियों का उद्देश्य: सैन्य शक्ति और जनकल्याण का संतुलन
अलाउद्दीन की बाजार नीतियाँ बहुआयामी थीं। प्राथमिक उद्देश्य था एक शक्तिशाली सेना का निर्माण, जिसमें लगभग 4.75 लाख सैनिक थे। सैनिकों का वेतन नकद था – एक घोड़े वाले सैनिक (एक अस्पा) को 234 टंका सालाना और दो घोड़े वाले (दो अस्पा) को 378 टंका। वेतन बढ़ाने से राजकोष पर बोझ पड़ता, इसलिए अलाउद्दीन ने आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित कर सैनिकों की क्रय शक्ति बनाए रखी। बरनी के अनुसार, “सुल्तान ने सस्ती कीमतों से सेना को मजबूत बनाया, ताकि मंगोलों का मुकाबला हो सके।”
दूसरा उद्देश्य आर्थिक स्थिरता था। दक्षिण विजयों से अपार धन आया, जिससे मुद्रा का मूल्य गिरा और महंगाई बढ़ी। अलाउद्दीन ने मांग-आपूर्ति को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति रोकी। तीसरा, जनकल्याण: अमीर खुसरो और बरनी (फतवा-ए-जहाँदारी में) ने इसे गरीबों के लिए बताया – “सामान्य जनता को सस्ती रोटी मिले।” फरिश्ता ने सुल्तान के 50,000 दासों के खर्च को कारण माना। कुल मिलाकर, ये नीतियाँ राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की मिसाल थीं, जो आधुनिक ‘प्राइस कंट्रोल’ और ‘रेशनिंग’ से मिलती-जुलती थीं। ऐतिहासिक रूप से, ये नीतियां अलाउद्दीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थीं।
क्रियान्वयन की आधारशिला: सूचना, भंडारण और राशनिंग
नीतियों की सफलता गुप्तचर तंत्र, राजकीय भंडार और राशन कार्ड पर टिकी थी।
अनाज संग्रह: दोआब क्षेत्र (गंगा-यमुना के बीच) और दिल्ली के आसपास के खालसा गांवों से लगान अनाज में लिया जाता था। झाइन क्षेत्र से आधा अनाज और आधा नकद। राजकीय गोदामों (अन्न-शालाएँ) में अनाज स्टॉक किया जाता, जो अकाल में वितरित होता।
राशनिंग प्रणाली: प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड जारी होता। प्रति व्यक्ति आधा मन अनाज मासिक। व्यक्तिगत संग्रह प्रतिबंधित – “कोई घर में अतिरिक्त अनाज न रखे।”
मूल्य निर्धारण: उत्पादन लागत + परिवहन + लाभ के आधार पर। उदाहरण:
| वस्तु | मूल्य (प्रति मन या अन्य इकाई) |
|---|---|
| गेहूं | 7.5 जीतल |
| चावल | 5 जीतल |
| घी | 1 जीतल प्रति 2.5 किलो |
| कपड़ा | सादा कपास 1-2 जीतल प्रति गज, रेशमी 10-500 टंका |
घोड़े: उत्तम 120 टंका, साधारण 10 टंका। कीमतों में आधा जीतल से अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होता था। यह प्रणाली राज्य की केंद्रीय नियोजन को दर्शाती है।
तीन प्रमुख बाजार: शहना-ए-मंडी, सराय-ए-अदल और पशु बाजार
अलाउद्दीन ने दिल्ली में तीन अलग-अलग बाजार स्थापित किए, प्रत्येक की देखरेख अलग अधिकारी करते थे।
- शहना-ए-मंडी (अनाज बाजार):
- स्थान: दिल्ली के मुख्य बाजार में।
- वस्तुएँ: गेहूं, चावल, दालें, घी, तेल।
- प्रबंधन: मलिक कबूल शहना-ए-मंडी थे। व्यापारी राजकीय गोदामों से अनाज लेते और निर्धारित दाम पर बेचते। राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता।
- विशेष: अकाल में प्रति घर आधा मन मुफ्त अनाज।
- सराय-ए-अदल (कपड़ा और विलास वस्तुओं का बाजार):
- स्थान: बदायूँ गेट के निकट खुले मैदान में।
- वस्तुएँ: कपड़े, शक्कर, जड़ी-बूटियाँ, मेवे, तेल।
- प्रबंधन: रायपरवाना प्रमुख। मुलतानी व्यापारी राज्य सहायता से माल लाते। अमीरों को बेशकीमती कपड़े निर्धारित दाम पर।
- कीमत रेंज: 1 टंका से 10,000 टंका तक।
- पशु, घोड़े और दास बाजार:
- दलालों पर प्रतिबंध – सीधे व्यापार।
- कीमतें: अच्छा घोड़ा 120 टंका, गाय 5 टंका, दास 10-20 टंका।
- उद्देश्य: सेना के लिए सस्ते घोड़े और पशु। इन बाजारों ने आर्थिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया।
अधिकारियों की भूमिका: दीवान-ए-रियासत और गुप्तचर तंत्र
- दीवान-ए-रियासत: नया विभाग, मलिक याकूब प्रमुख। मूल्य नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी। व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य – नाम, माल, जमानत।
- शहना-ए-मंडी: प्रत्येक बाजार का अधीक्षक।
- गुप्तचर: बरीद (संदेशवाहक) और मुनहियान (व्यक्तिगत जासूस) बाजार घूमते। सुल्तान को दैनिक रिपोर्ट।
- मुहतसिब: नैतिक पुलिस, माप-तौल की जाँच।
- नाजिर: वजन निरीक्षक। व्यापारी सराय-ए-अदल में माल लाने की शपथ लेते। यह तंत्र आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों से मिलता-जुलता था।
दंड व्यवस्था: कठोरता की मिसाल
उल्लंघन पर क्रूर दंड:
- काला बाजारी: कोड़े, जुर्माना, निर्वासन।
- कम वजन: उतना ही मांस शरीर से काटा जाता।
- मिलावट: दुकान जब्त, मारपीट। बरनी लिखता है, “कीमतें इतनी स्थिर कि आधा जीतल का अंतर नहीं।” यह कठोरता नीतियों की सफलता का आधार थी।
नीतियों का प्रभाव और मूल्यांकन
सकारात्मक: सेना मजबूत हुई, मंगोल रोके गए। गरीबों को सस्ती वस्तुएँ। महंगाई नियंत्रित। आर्थिक केंद्रीकरण से राज्य मजबूत।
नकारात्मक: व्यापारियों पर दबाव, काला बाजार बढ़ा। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मुबारकशाह ने समाप्त कीं।
ऐतिहासिक महत्व: यह प्राचीन भारत में पहली ‘नियोजित अर्थव्यवस्था’ थी। मोरलैंड और इरफान हबीब जैसे विद्वान इसे ‘सोशलिस्ट’ तत्वों वाला बताते हैं। सक्सेना और लाल के अनुसार, केवल दिल्ली तक सीमित, लेकिन प्रभावी। इन नीतियों ने अलाउद्दीन को एक आर्थिक सुधारक के रूप में स्थापित किया।
खिलजी वंश की कला और वास्तुकला
खिलजी युग (1290–1320 ई.) की कला और इमारतें दिल्ली के स्थापत्य में इंडो-इस्लामिक और फारसी मिश्रण दिखाती हैं। ये दुर्ग, मस्जिदें, जलाशय और द्वारों पर केंद्रित रहीं।
सीरी 1303 ई. में बनी सीरी दिल्ली की सात मध्यकालीन नगरीयों में दूसरी थी। यहां राजमहल, बाजार और भव्य भवन थे। अलाउद्दीन का ‘कसर-ए-हजार सतून’ महल हजार स्तंभों वाला प्रसिद्ध था।
अलाई मीनार 1311 में अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंची मीनार शुरू की, लेकिन 1316 में उनकी मृत्यु से सिर्फ पहला तल पूरा हुआ। आज यह रबड़ मलबे का ढेर है।
अलाई दरवाजा लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना, कुतुब परिसर का मुख्य द्वार। घोड़े की नाल आकार के मेहराब, उभरा गुंबद और ज्यामितीय नक्काशी वाली यह इंडो-फारसी कला का उदाहरण है।
जमात-खाना मस्जिद अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान द्वारा बनी, निजामुद्दीन औलिया की मजार के पश्चिम। तीन कमरों वाली, इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित। लाल पत्थर से बनी, बाद में तुगलकों ने विस्तार किया। दीवारों पर कुरान आयतें और पैटर्न।
हौज-ए-अलाई 1305 ई. में सीरी में 70 एकड़ का जलाशय, मानसून पानी से भरता। शहर की पानी आपूर्ति का स्रोत।
अलाउद्दीन का मदरसा और मकबरा 1315 में बना, भारत में पहला जहां मकबरा और मदरसा एक साथ। 11वीं-12वीं सदी की सल्जुक परंपरा से प्रेरित, चौकोर आंगन के चारों ओर एल-आकार।
स्रोत-विकिपीडिया
खिलजी वंश: सामान्य प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1: खिलजी वंश की स्थापना किसने की?
जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ई. में मामलूक वंश को हटाकर खिलजी राजवंश शुरू किया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अफगान मूल के शासकों की नींव रखी।
प्रश्न 2: खिलजी वंश के मुख्य शासक कौन थे?
इस वंश में तीन प्रमुख शासक हुए: जलालुद्दीन खिलजी (1290-1296 ई.), अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316 ई.) और मुबारक शाह खिलजी (1316-1320 ई.)। अलाउद्दीन सबसे शक्तिशाली थे।
प्रश्न 3: दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है?
अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को ‘सिकंदर-ए-सानी’ कहा, क्योंकि उनकी सैन्य विजयें भारत के बड़े हिस्से तक फैलीं और वे महत्वाकांक्षी योद्धा थे।
प्रश्न 4: गाजी मलिक कौन थे?
गाजी मलिक अलाउद्दीन के समय एक सेनापति थे, जो बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक बने। उन्होंने 1320 ई. में तुगलक वंश की शुरुआत की।
प्रश्न 5: खिलजी वंश को किसने हराया?
ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 ई. में मुबारक शाह को पराजित कर खिलजी शासन समाप्त किया और नया तुगलक राजवंश स्थापित किया।