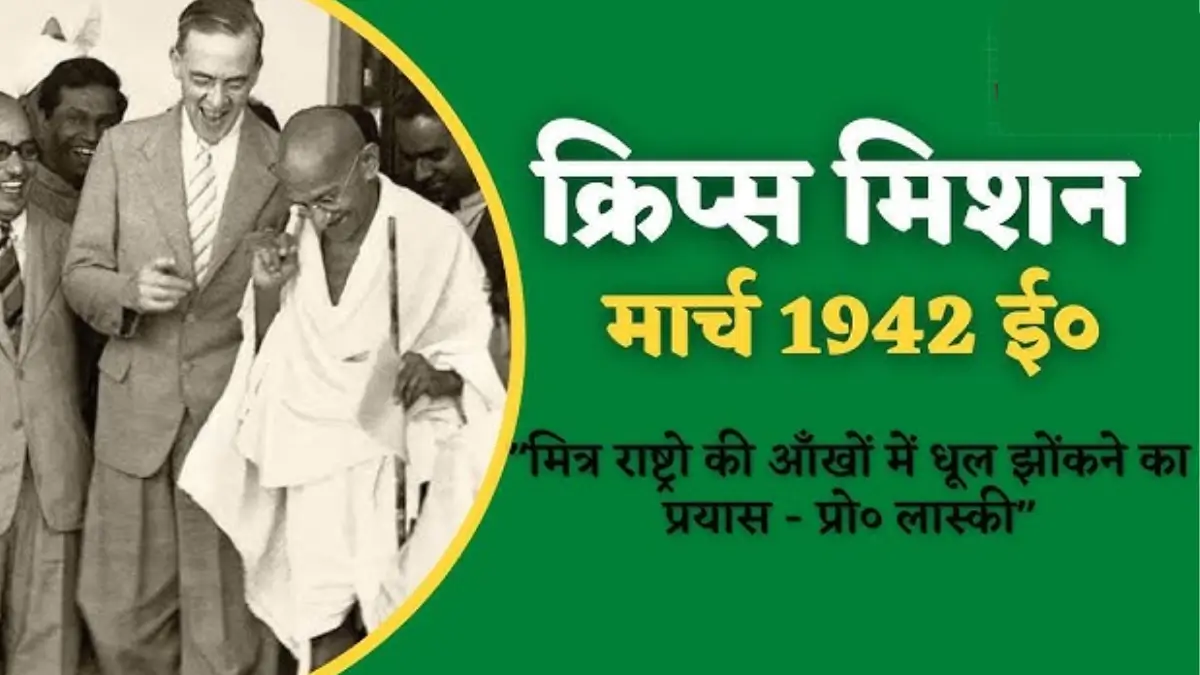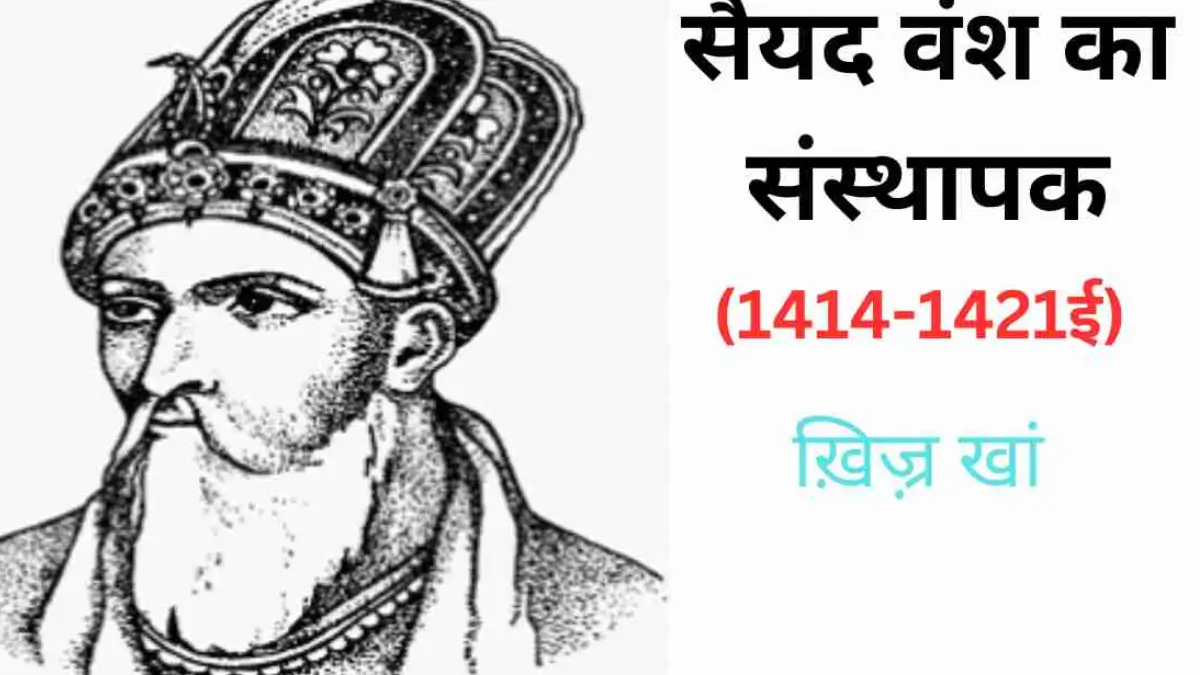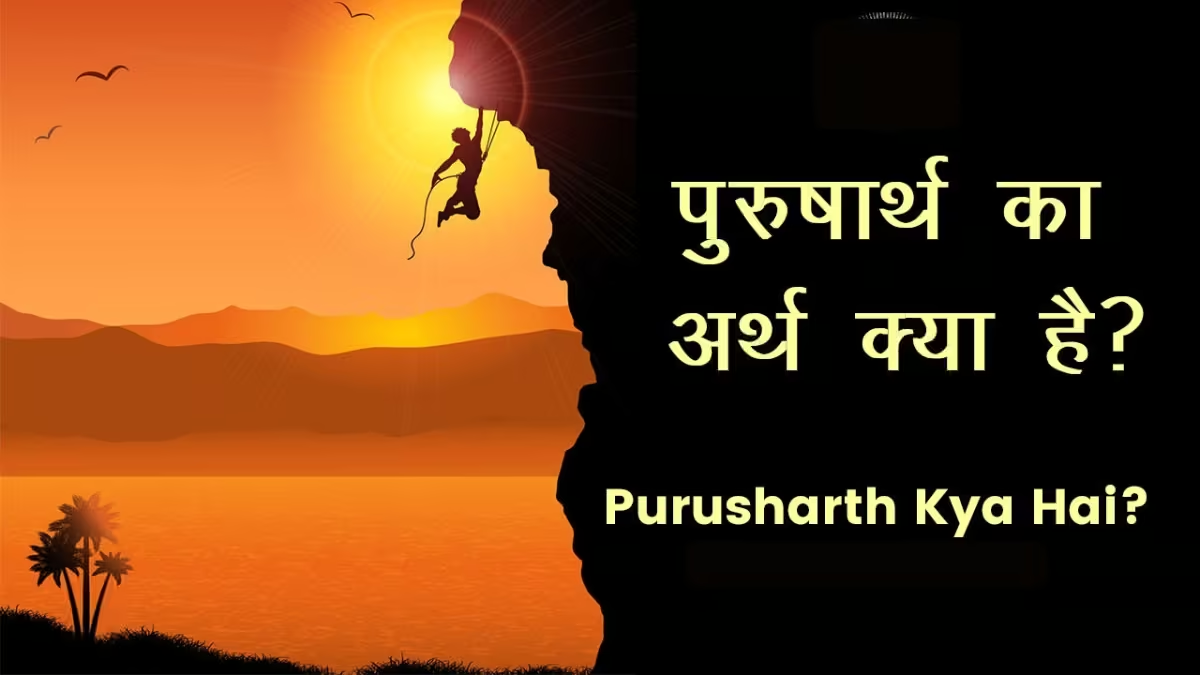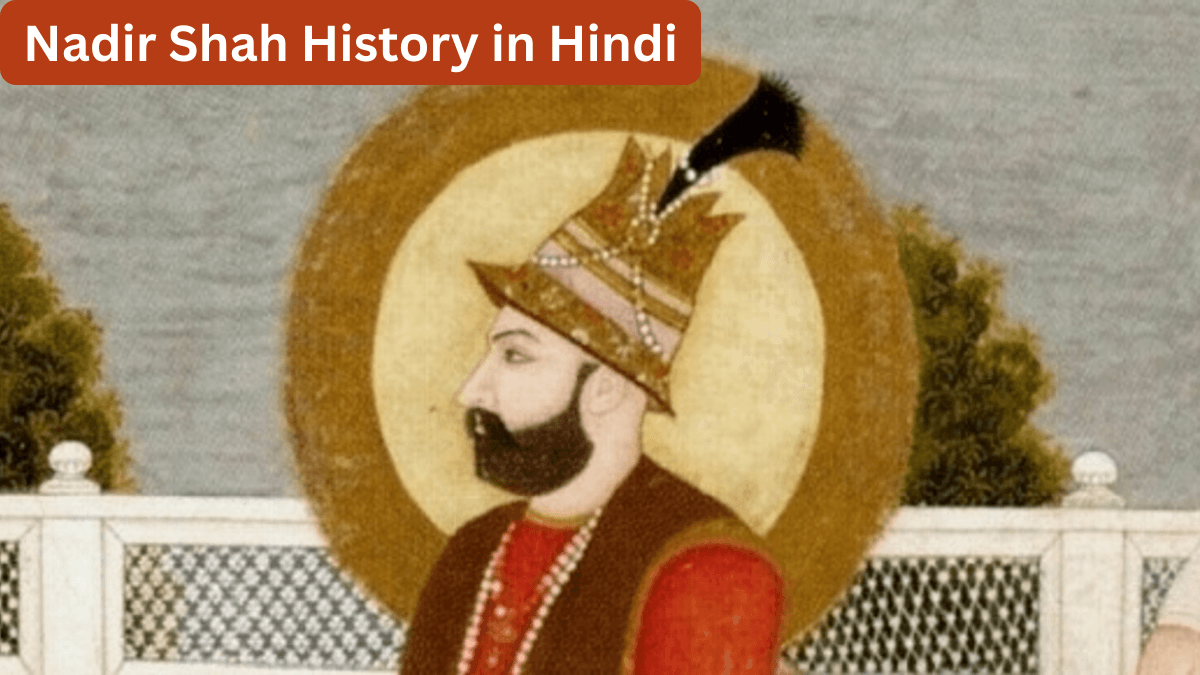भारत में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के लिए असंख्य क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मगर एक क्रन्तिकारी जिसने सबसे ज्यादा अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा और ऐसी वीरता दिखाई जो पहले किसी ने नहीं दिखाई थी। जी हाँ हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, एक ऐसा युवा क्रन्तिकारी जिसने काम आयु में ही हँसते-हँसते फांसी को फंदे पर लटकाना मंजूर किया मगर अंग्रेजों से माफ़ी माँगन स्वीकार नहीं किया।
जब भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की बात होती है तो भगत सिंह का स्थान सर्वोपरि है। शहीद भगत सिंह हमारे देश के महानतम क्रांतिकारियों में से एक हैं, ऐसे वीर, साहसी, निडर क्रांतिकारी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम आज का लेख भगत सिंह का जीवन परिचय: जन्मदिन, स्वतंत्रता संग्राम, निबंध, पुण्यतिथि, प्रेरक शब्द,और शहीद दिवस | Bhagat Singh Biography in Hindi में भगत सिंह के जीवन से जुड़े विभिन्न घटनाओं पर चर्चा करेंगे। लेख को अंत तक अवश्य पढ़े
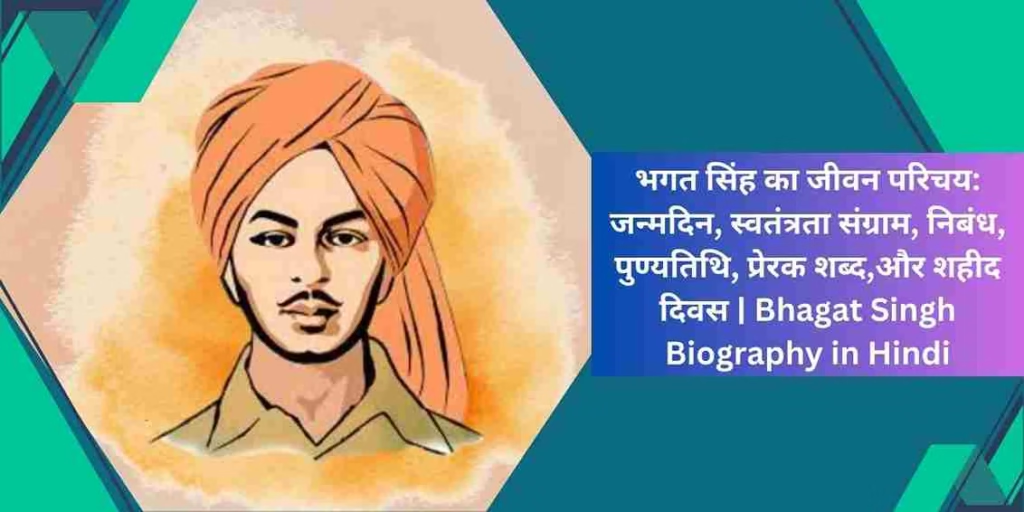
| नाम | भगत सिंह |
| पूरा नाम | सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह |
| जन्म | 28 सितम्बर 1907 अथवा 19 अक्टूबर 1907 ई. |
| जन्मस्थान | चक बंगा,जारनवाला तहसील, पंजाब (वर्तमान पाकिस्तान) |
| पिता | सरदार किशन सिंह |
| माता | विद्यावती कौर |
| भाई | रणवीर, कुलतार, राजिंदर, कुलबीर, जगत |
| बहन | प्रकाश कौर, अमर कौर, शकुंतला कौर |
| पुस्तक | मैं नास्तिक क्यों हूँ |
| योगदान | स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों का |
| फांसी | 23 मार्च 1931, लाहौर |
भगत सिंह का परिचय (Bhagat Singh Biography in Hindi)
निस्संदेह देश की स्वतंत्रता का नेतृत्व कांग्रेस और महत्मा गाँधी के हाथों में था और आज़ादी के प्रारम्भिक प्रयास तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल थे। लेकिन निरंतर उपेक्षा और ढुलमुल रवैये ने देश में एक क्रन्तिकारी युवा समूह को जन्म दिया जो राजनीतिक हिंसा में विश्वास करता था और अपनी भाषा में ब्रिटिश शासन को जवाब देने के लिए उत्सुक था।
उत्तर भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह सभी युवाओं के लिए युवा प्रतीक थे, जिन्होंने उन्हें देश के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। भगत सिंह एक सिख परिवार में पैदा हुए एक निडर युवा थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। उन्होंने क्रांतिकारी युवाओं का मार्गदर्शन किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसे युवा वर्ग का निर्माण किया जो मौत से नहीं डरता था। भगत सिंह का सम्पूर्ण जीवन क्रन्तिकारी संघर्ष और आजादी की कहानियों से भरा है, आज के युवा भी उनके जीवन और आजादी के संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन राष्ट्रवाद का एक पूरा अध्याय है।
भगत सिंह का बचपन (Early life of Bhagat Singh)
भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव, जारवाला तहसील पंजाब (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था जो एक किसान थे। माता का नाम विद्यावती कौर था जो एक गृहणी थीं। इसके अलावा उनके परिवार में भाई रणवीर, कुलतार, राजिंदर, कुलबीर, जगत तथा बहनें प्रकाश कौर, अमर कौर, शकुंतला कौर थीं। भगत सिंह बचपन से ही एक अलग प्रवृत्ति के थे और उनमें क्रन्तिकारी गुण प्रारम्भ से ही झलकते थे।
भगत सिंह की शिक्षा
भगत सिंह ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा दयानंद एंग्लो-वैदिक हाई स्कूल से प्राप्त की और फिर आगे की पढाई लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की। उस समय विवाह जल्दी होते थे और युवा भगत सिंह के माता-पिता भी उनकी शादी जल्दी करना चाहते थे मगर उन्होंने अपने माता पिता से शादी के लिए स्पष्ट इंकार कर दिया मगर जब परिवार ने ज्यादा जोर डाला तो वे घर छोड़कर चले गए और कहा कि उनकी दुल्हन सिर्फ मौत होगी।
जलियावाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919)
पंजाब क्रन्तिकारी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने इन पर काबू पाने के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पंजाब में मार्शल लौ लगा दिया। इस सैनिक कानून के तहत पंजाब के दो क्रन्तिकारी डॉ. सतपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
इस घटना के विरोध में पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला गया और यह भीड़ अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एकत्र हुई। तभी पंजाब का सैन्य कमांडर जरनल डायर जिसका पूरा नाम कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर था ने वहां पहुंचकर भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी करा दी। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने युवा भगत सिंह को अंदर तक झकझोर दिया।
भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन में क्यों शामिल हुए?
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में हुए जलियाँवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह के युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़ाई बेच में छोड़कर भगत सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत लाहौर में जॉन सैंडर्स की हत्या और फिर दिल्ली की केंद्रीय संसद (सेंट्रल असेंबली) में बम विस्फोट ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ खुले विद्रोह का अलार्म खड़ा कर दिया।
जब भगाता सिंह ने सेंट्रल असेम्बली में बम फेंका तो उन्होंने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 23 मार्च, 1931 को उनके दो अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फाँसी दे दी। सन् 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में चौरी-चौरा हत्याकांड (जिसमें 14 पुलिसकर्मियों की जलाकर मौत हुई थी) के बाद जब गांधी जी ने किसानों का समर्थन नहीं किया तो भगत सिंह बहुत निराश हुए।
उसके बाद, गांधी और अहिंसा के सिद्धांत से उनका विश्वास कमजोर हो गया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। इसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बने गदर दल में शामिल हो गए।
काकोरी कांड और भगत सिंह की प्रतिक्रिया – हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का गठन
काकोरी कांड में (जिसमें ट्रेन रोककर ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था) भगत सिंह, राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ सहित 04 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास से इतने व्याकुल थे कि वे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अपनी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सहित एक नए क्रन्तिकारी संगठन ‘हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ का गठन किया। इस क्रन्तिकारी संगठन का उद्देश्य राष्ट्र सेवा, त्याग और कष्ट सहने के योग्य युवकों को तैयार करना था।
जॉन सैंडर्स की हत्या
भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर, 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या को अंजाम दिया था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को अंजाम देने में उनकी पूरी मदद की थी।
सेंट्रल असेंबली में बम कांड
भगत सिंह ने साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के कानों तक आज़ादी की आवाज़ पहुँचाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के ऑडिटोरियम, वर्तमान नई दिल्ली में, संसद भवन में बम और पर्चे फेंके थे। हालाँकि बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, फिर भी ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए केबल फेंकी गई थी। बम फेंकने के बाद दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
क्रांतिकारी गतिविधियाँ – भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह 12 वर्ष के थे। इस हत्याकांड की सूचना पाकर 12 वर्षीय भगत सिंह स्कूल छोड़कर बारह मील दूर पैदल जलियांवाला पहुंचे। इस समय भगत सिंह अपने चाचा के क्रांतिकारी साहित्य को पढ़कर हिंसा के सिद्धांत को लेकर भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हिंसा और अंहिंसा में से किसका चुनाव करें।
अब भगत सिंह को महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन और क्रांतिकारियों की हिंसक कार्रवाइयों में से किसी एक को चुनना था। हालाँकि भगत सिंह के मन में गांधी के प्रति बहुत सम्मान था, लेकिन असहयोग आंदोलन (1920-22) के अचानक समाप्त हो जाने के कारण वे नाराज थे। अब उन्होंने गांधीजी के अहिंसक सिद्धांत के स्थान पर स्वतंत्रता के लिए हिंसक क्रांति का मार्ग अपनाना उचित समझा।
भगत सिंह स्वतंत्रता के जुलूसों में भाग लेने लगे और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बन गए। उनके प्रमुख क्रांतिकारी साथियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु सबसे साहसी थे। काकोरी कांड (9 अगस्त, 1925 ) की घटना के बाद इस रेल लूट में गिरफ्तार 4 क्रांतिकारियों (राजेन्द्र लाहिडी, अशफाक उल्ला खाँ, पण्डित राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ एवं ठाकुर रोशनसिंह) को मौत की सजा (22 अगस्त1927) और 16 अन्य को अलग-अलग धाराओं में कारावास की सजा सुनाई गई ।भगत सिंह इस घटना से इतने व्यथित थे कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया और इसे एक नया नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया।
लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध
1928 में साइमन कमीशन भारत आया, पूरे भारत में बहिष्कार और प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 को भारत आए, साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें पंजाब के क्रन्तिकारी नेता लाला लाजपत राय भी उनके साथ थे। वे लाहौर रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर “साइमन गो बैक” के नारे लगाते रहे। जिसके बाद वहां पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हो गए. ब्रिटिश सरकार ने इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया।
इस बर्बर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु (17 November 1928) हो गई। यह घटना भगत सिंह के लिए यह असहनीय थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गुप्त योजना के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। रणनीति के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त और अज्ञात मुद्रा में चलने लगे। उधर, जयगोपाल अपनी साइकिल से उतकर ऐसे उठा कर बैठ गए जैसे वह टूट गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सतर्क हो गए। उधर, चंद्रशेखर आजाद पास के डीएएलवी विद्यालय की चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में गार्ड की भूमिका में थे।
सांडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928
जैसे ही ए.एस.पी. सॉन्डर्स 17 दिसंबर 1928 को सुबह लगभग 4.00 बजे पहुंचे, राजगुरु ने सीधे उनके सिर में गोली मार दी और उनकी वहीं मौत हो गई। गुस्से से भरे भगत सिंह ने भी 3-4 गोलियां चलाकर उनकी मौत का पूरा इंतजाम कर दिया। जैसे ही ये दोनों भाग रहे थे, एक भारतीय सैनिक चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे चेतावनी देते हुए कहा – “अगर वह आगे बढ़ा तो मैं उसे गोली मार दूंगा।” लेकिन वह नहीं रुका और आजाद ने उसे गोली मार दी और वह वहीं मर गया। इस प्रकार इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया।
केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना 8 अप्रैल, 1929
हालांकि भगत सिंह रक्तपात के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वे वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते थे और उसी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। हालांकि, वह एक कट्टर समाजवादी थे। बाद में उनके विरोधी उन पर अपनी विचारधारा बताकर भगत सिंह के नाम पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाते रहे हैं।
सेंट्रल असेंबली में बम की योजना क्यों बनाई गई थी
कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिला पाई, क्योंकि उन्होंने युवाओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने के लिए भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल किया। भगत सिंह पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति को नापसंद करते थे। उस समय चूंकि अंग्रेज सर्वेसर्वा थे और बहुत कम भारतीय उद्योगपति ही आगे बढ़ पाते थे, इसलिए मजदूरों के प्रति अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना उनके लिए स्वाभाविक था।
मजदूर विरोधी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित नहीं होने देना उनके समूह का निर्णय था। सब चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चले कि भारतीय जाग गए हैं और उनके मन में ऐसी नीतियों के प्रति रोष है। ऐसा करने के लिए उसने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी।
भगत सिंह बिना किसी खून-खराबे के अंग्रेजों के कानों तक ‘आवाज’ पहुंचाना चाहते थे। हालाँकि शुरू में उनके साथी सहमत नहीं थे, लेकिन अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नाम सुझाए गए। तय कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेम्बली के खाली स्थान पर बम फेंका गया ताकि किसी को चोट न लगे, पूरा हॉल धुएँ से भर गया। भगत सिंह ने भागने के बजाय गिरफ्तारी स्वीकार कर ली, चाहे उन्हें फांसी ही क्यों न दी जाए। उस वक्त दोनों खाकी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे।
बम फटने के बाद उन्होंने “इंकलाब-जिंदाबाद, साम्राज्यवाद-मुर्दाबाद!” और अपने साथ लाए हुए पत्रों को हवा में उछाल दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
जेल में भगत सिंह के दिन (8 अप्रैल 1929 -23 मार्च 1931)
भगत सिंह ने लगभग 2 साल जेल में बिताए। इस दौरान उन्होंने अपने विचारों को शब्दों में ढाला और जेल में रहते हुए भी कई अन्य विचारकों और दार्शनिकों को पढ़ा। उस दौरान उनके रिश्तेदारों को लिखे गए उनके लेख और पत्र आज भी उनके विचारों को दर्शाते हैं।
भगत सिंह ने अपनी रचनाओं में पूंजीपतियों को कई तरह से अपना दुश्मन बताया है। वे लिखते हैं कि “मजदूरों का शोषण करने वाला हर पूंजीपति उनका दुश्मन है, भले ही वह भारतीय ही क्यों न हो”। उन्होंने जेल में ‘मैं नास्तिक क्यों हूं’ शीर्षक से अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था। जेल में रहते हुए भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास की भूख से मृत्यु हो गई।
भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा
इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर 26 अगस्त, 1930 को अदालत में मुकदमा चला और औपचारिक रूप से उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 एफ और आईपीसी की धारा 120 के तहत दोषी ठहराया।
7 अक्टूबर, 1930 को अदालत ने 68 पन्नों में अपना फैसला सुनाया, फैसले के मुताबिक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही दंगे की आशंका में लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। भगत सिंह की मौत की सजा को माफ करने के लिए प्रिवी काउंसिल में एक असफल अपील की गई, जिसे 10 जनवरी, 1931 को खारिज कर दिया गया।
इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पं. मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रयासों से 14 फरवरी, 1931 को वायसराय के सामने क्षमादान की अपील दायर की और वायसराय के विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए मानवीय आधार पर क्षमा की मांग की।
गांधीजी ने 17 फरवरी, 1931 को फांसी की सजा माफ करने के लिए वायसराय से बात की, फिर 18 फरवरी, 1931 को आम जनता ने भी वायसराय से गुहार लगाई। ये सारे प्रयास भगत सिंह की इच्छा के विरुद्ध किए जा रहे थे क्योंकि भगत सिंह माफी नहीं चाहते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने यही शर्त रखी कि भगत सिंह माफीनामा लिखकर दें। मगर भगत सिंह ने स्पष्ट रूप से माफ़ी मांगें से इंकार कर दिया था।
भगत सिंह की फांसी का दिन 23 मार्च 1931
आखिर वह दुखद दिन आया और 23 मार्च, 1931 को शाम करीब 7:33 बजे भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फाँसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें लेनिन की पूरी जीवनी पढ़ने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जब जेल अधिकारियों ने उन्हें बताया कि फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा था – “रुको! पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिलें।” फिर एक मिनट के बाद किताब छत की तरफ उछली और बोले- “अच्छा अब चलते हैं।”
फाँसी के तख्ते पर जाते समय वे तीनों निडरक्रन्तिकारी मस्त होकर मजे में गा रहे थे –
रंग दे बसंती चोला, रंग दे।
मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग बसंती चोला दे।
ब्रिटिश सरकार इस बात से डरी हुई थी की फांसी की खबर से दंगें न भड़क जाएँ। इसके बाद अंग्रेजों ने वह क्रूरतम तरीका अपनाया जिसे सुनकर रूह काँप जाये, अंग्रेजों ने पहले मृत क्रांतिकारियों के शव के टुकड़े-टुकड़े किए, फिर बोरियों में भरकर फिरोजपुर ले गए, जहां घी की जगह मिट्टी का तेल डालकर चुपके से उनके विछिप्त शवों को जला दिया गया। आग जलती देख ग्रामीण आ गए और अंग्रेजों ने उनके शव के अधजले टुकड़े सतलुज नदी में फेंक दिए और भाग गए। ग्रामीणों ने शहीदों के अधजले टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत अंतिम संस्कार किया। इस तरह भगत सिंह सहित सभी क्रांतिकारी हमेशा के लिए अमर हो गए।
जवाब में, भारतीयों ने उनकी मृत्यु के लिए अंग्रेजों के साथ-साथ गांधी को भी दोष देना शुरू कर दिया। जब गांधीजी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने काले झंडों से गांधीजी का स्वागत किया। कुछ जगहों पर गांधी पर हमले भी हुए, लेकिन सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने उन्हें बचा लिया।

भगत सिंह की प्रसिद्धि और सम्मान
भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की खबर लाहौर के डेली ट्रिब्यून और न्यूयॉर्क के एक अखबार डेली वर्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्र-पत्रिकाओं में उन पर लेख प्रकाशित हुए, लेकिन भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध होने के कारण भारतीय बुद्धिजीवियों और जनता को इसकी जानकारी नहीं थी। उनकी शहादत को देश भर में याद किया गया।
दक्षिण भारत में पेरियार अपने लेख “मैं नास्तिक क्यों हूँ?” के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन 22-29 मार्च 1931 के अपने साप्ताहिक पत्र कुदाई आरसु के अंक में तमिल में एक संपादकीय लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई और उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर जीत के रूप में देखा गया।
यह भी पढ़िए– औरंगजेब का मकबरा किसने बनवाया था | Tomb of Aurangzeb History In Hindi
आज भी भारत और पाकिस्तान के लोग भगत सिंह को एक ऐसे स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपनी जवानी सहित अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। भगत सिंह का पुश्तैनी घर आज भी पाकिस्तान में संरक्षित है और उनकी मूर्तियां पाकिस्तान में कई जगह आज भी लगी हुई हैं। भगत सिंह का जीवन युवाओब के लिए आदर्श है मगर अफसोजनक यह है कि लोग भगत सिंह को तो स्वीकार करते हैं मगर उनकी विचारधारा को याद नहीं करते। उनके जीवन ने कई हिंदी फिल्म पात्रों को प्रेरित किया।
जन्मतिथि विवाद और भगत सिंह का नाम भगत क्यों रखा गया?
भगत सिंह की जन्म तिथि चर्चा का विषय है। इनका जन्म अधिकतर 28 सितम्बर 1907 को माना जाता है। लेकिन भगत सिंह का जन्म पंजाब के गाँव बंगा, तहसील जादनवाला, जिला लायलपुर (वर्तमान पाकिस्तान) में शक संवत 1964 की आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि को शनिवार (तदनुसार 19 अक्टूबर, 1907 ई.) को प्रातः 9:00 बजे हुआ था।
उनके जन्म के दिन ही बंगा तक यह खबर पहुंच गई थी कि सरदार अजीत सिंह आजाद (भगत सिंह के चाचा) हो गए हैं और भारत लौट रहे हैं। घर में खबर भी पहुँची कि सरदार कृष्ण सिंह जी नेपाल से लाहौर पहुँचे हैं और सरदार सुवर्ण सिंह जी उसी दिन जेल से रिहा होकर घर पहुँचे। जहां भगत सिंह की दादी ने अपने पोते का चेहरा देखा वहीं उन्हें भी अपने तीन बिछड़े बेटों की खुशखबरी मिली।
तो उन्होंने कहा कि बच्चे का जन्म ‘भागोंवाला’ (भाग्यशाली) हुआ था, इसीलिए बच्चे का नाम बाद में भगत सिंह रखा गया। 23 मार्च, 1931 को उनकी शहादत के तुरंत बाद भगत सिंह पर केंद्रित ‘अभ्युदय’ पत्रिका के लिए विशेष रूप से लिखी गई ‘फरिश्ता भगत सिंह’ शीर्षक की प्रस्तावना में भी इसी जन्म तिथि को स्वीकार किया गया है।
इतना ही नहीं, 16 अप्रैल 1931 को प्रकाशित भविष्य पत्रिका के अंक में भगत सिंह की प्रस्तावना में भी यही जन्मतिथि दी गई है।
पुन: 4 जून, 1931 को प्रकाशित ‘भविष्य’ अंक में भगत सिंह के घनिष्ठ मित्र श्री जितेंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित जीवनी के भाग में भगत सिंह का जन्म अक्टूबर 1907 में सुबह शनिवार को माना जाता है।
क्रांतिकारी दल में स्वयं शामिल रहे सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री मन्मथनाथ गुप्त ने भी उक्त तिथि को स्वीकार किया है।
इस प्रकार भगतसिंह के समकालीन व्यक्तियों द्वारा वर्णित तथ्यों के अनुसार उनकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1907 ई. ही सिद्ध होती है। इतना होते हुए भी इनकी जन्म तिथि 28 सितम्बर प्रचलित हुई है और इन पर कार्य करने वाले विद्वान भी बिना किसी विशेष विचार के 28 सितम्बर को इनकी जन्मतिथि मान रहे हैं।
यह भी पढ़िए-
| कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत: | महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण |
| मुहम्मद बिन कासिम: भारत पर आक्रमण | औरंगज़ेब का इतिहास: |
भगत सिंह के अनमोल बचन
1. मेरे ताप से राख का कण-कण थरथरा रहा है, मैं ऐसा दीवाना हूं कि जेल में भी आजाद हूं।
2. यह जरूरी नहीं कि क्रांति में हमेशा संघर्ष ही हो। यह रास्ता बम और पिस्टल का नहीं है।
3. उन्नति के मार्ग में बाधक बनने वाले व्यक्ति को परम्परागत प्रवृत्ति की आलोचना और विरोध करने के साथ-साथ उसे चुनौती भी देनी होगी।
4. मैं मानता हूं कि मैं महत्वाकांक्षी, आशावादी और जीवन के प्रति उत्साही हूं, लेकिन मैं जरूरत के हिसाब से इन सबका त्याग कर सकता हूं, यही सच्चा त्याग होगा।
5. किसी भी कीमत पर बल का प्रयोग न करना एक काल्पनिक आदर्श है और देश में जो नया आंदोलन शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत हमने गुरु गोबिंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और राजा खान, वाशिंगटन और गैरीबाल्डी, लाफायेते को दी थी। और लेनिन के आदर्शों का पालन किया जाता है।
6. कोई व्यक्ति तभी कोई कार्य करता है जब वह अपने कार्य के परिणाम को निश्चित (न्यायसंगत) करता है जैसे हम तब थे जब हमने सभा में बम फेंका था।
7. निर्भीकता और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दो गुण हैं।
8. मैं एक इंसान हूं और मुझे उन चीजों की परवाह है जो मानवता को प्रभावित करती हैं।
9. ज़िंदगी अपने आप चलती है… आख़िरी सफ़र दूसरो के कंधों पर पूरा होता है।
10. प्रेमी, पागल और कवि एक ही थाली में होते हैं, अर्थात समान होते हैं।
11. अगर बहरा सुनना चाहता है तो आवाज उठानी होगी। जब हमने बम फेंका तो हमारा इरादा किसी को मारने का नहीं था। हमने ब्रिटिश सरकार पर बम फेंका। ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर स्वतंत्र होना पड़ेगा।
12. किसी को “क्रांति” को परिभाषित नहीं करना चाहिए। इस शब्द के कई अर्थ और अर्थ हैं जो इसके उपयोग या दुरुपयोग को तय करते हैं।
13. आमतौर पर लोग परिस्थिति के अभ्यस्त हो जाते हैं और उनमें बदलाव करने के विचार मात्र से ही डर जाते हैं। इसलिए हमें इस भावना को क्रांति की भावना से बदलने की जरूरत है।
14. क्रांति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, साथ ही स्वतंत्रता भी जन्मसिद्ध अधिकार है और परिश्रम वास्तव में समाज को आगे बढ़ाता है।
15. अहिंसा में आत्मविश्वास की शक्ति होती है जिसमें विजय की आशा से दुखों को सहन किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर यह प्रयास विफल हो जाए? फिर हमें इस आत्मिक शक्ति को भौतिक शक्ति (शारीरिक सजक्ति) के साथ जोड़ना होगा ताकि हम अत्याचारी शत्रु की दया पर न रहें।
16. व्यक्तियों को कुचल कर वे विचारों को नहीं मार सकते।
17. कानून की पवित्रता तभी तक कायम रह सकती है जब तक वह लोगों की इच्छा को दर्शाता है।
18. अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो निजी संपत्ति किसी को नहीं मिलेगी.
19. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, यह एक सजा है।
21. प्रेमी, दीवाना और कवि एक ही चीज से बने हैं।
22. जो विकास के लिए खड़ा है उसे आलोचना करनी चाहिए, अविश्वास करना चाहिए और हर रूढ़िवादी चीज को चुनौती देनी चाहिए।
23. क्रान्ति में आवश्यक रूप से अभिशप्त संघर्ष शामिल नहीं था। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था।
24. “बहरों के कानों तक आवाज पहुँचाने के लिए, आवाज बहुत तेज होनी चाहिए, केंद्रीय अस्सेम्बली में बम फेंकते समय, हमारा उद्देश्य किसी की हत्या होकर, ब्रिटिश हुकूमत के कानों तक आवाज पहुँचाना था.
25. “क्रांति शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और इसका शाब्दिक अर्थ नहीं करना चाहिए, स्वार्थी लोग अपने फायदे के लिए इसके अलग-अलग अर्थ निकालते हैं।”
26. “मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं जीवन के प्रति महत्वाकांक्षा, आशा और आकर्षण से भरा हूं और यही सच्चा बलिदान है।”
27. “जब लोग चीजों आदि हो जाते हैं, तब बदलाव उन्हें भयभीत कर देता है। इस भय और निष्क्रता को क्रांति में परिवर्तित करना है।”
28. “बम और पिस्तौल जैसे हथियार क्रांति के प्रतीक नहीं हैं, क्रांति तो विचारों की एक तेज धार वाली तलवार होती है।”
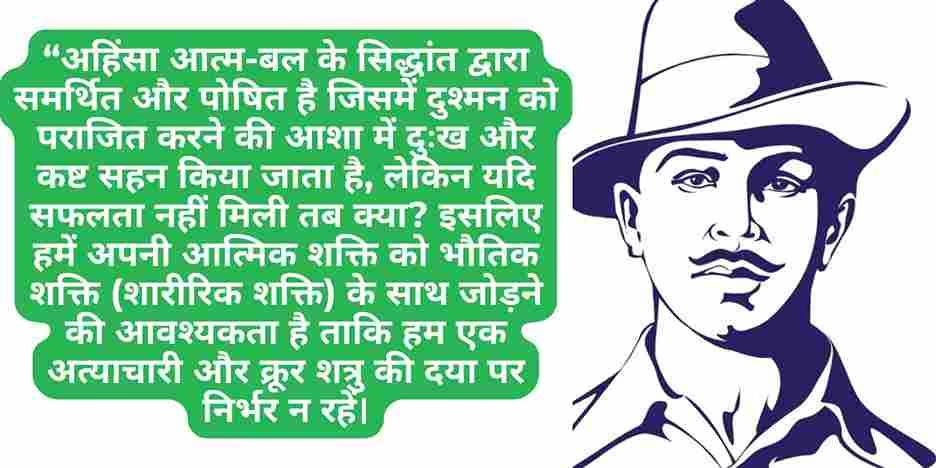
29. “क़ानून की पवित्रता का अस्तित्व तभी तक है जब तक वह लोगों के इच्छानुसार काम करता है।”
30. “मनुष्य तभी कुछ करने में सफल होता है जब वह अपने कार्य के औचित्य के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त होता है, जैसे कि हम सभा में बम फेंकने वाले थे।”
31 . “निर्मम आलोचना और मुक्त विचार क्रांतिकारी सोच की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।”
32 . यदि धर्म को एक तरफ रखा जाए तो हम सब राजनीति पर एक हो सकते हैं। हम धर्मों में अलग रह सकते हैं।
भगत सिंह के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-FAQs
प्रश्न- भगत सिंह का नारा कौन सा है?
उत्तर– “इंक़लाब ज़िन्दाबाद“, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रेल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक़्त इसे बुलंद किया था।
प्रश्न- भगत सिंह को फांसी कब और कहाँ दी गई थी?
उत्तर- 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई
प्रश्न- भगत सिंह के माता-पिता का नाम क्या था?
उत्तर- भगत सिंह के माता-पिता नाम विद्यावती कौर और सरदार किशन सिंह था।
प्रश्न- भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है?
उत्तर- चक बंगा,जारनवाला तहसील, पंजाब (वर्तमान पाकिस्तान) में भगत सिंह का जन्म 28 सितम्बर 1907 को हुआ
प्रश्न- भगत सिंह का केस किसने लड़ा?
उत्तर- भगत सिंह का केस आसफ़ अली ने लड़ा था।
प्रश्न- भगत सिंह की पत्नी का क्या नाम है?
उत्तर- भगत सिंह ने विवाह नहीं किया था। जिन दुर्गा देवी का नाम लिया जाता है वे भगत सिंह के साथी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थीं और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उन्होंने भगत सिंह की पत्नी की भूमिका निभाई।
प्रश्न- भगत सिंह ने कितनी पढ़ाई की थी?
उत्तर- भगत सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई दयानंद एंग्लो-वैदिक हाई स्कूल में की और फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में आगे की पढ़ाई की.
अगर आपको इतिहास पढ़ना पसंद है तो ये भी पढ़िए
- समुद्रगुप्त का जीवन परिचय और उपलब्धियां
- मुगल सम्राट अकबर: जीवनी,
- सती प्रथा किसने बंद की:
- मुगल शासक बाबर का इतिहास: एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता
- रूसी क्रांति 1917: इतिहास, कारण और प्रभाव
- पुष्यमित्र शुंग का इतिहास और उपलब्धियां
- नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं और स्थल: एक विस्तृत अध्ययन
- Firuz Shah Tughlaq History in Hindi: प्रारम्भिक जीवन, माता-पिता,